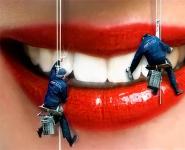प्राचीन दर्शन. प्राचीन विश्व के दर्शन के उद्भव का इतिहास
प्राचीन यूनानी दर्शन यूनानी संस्कृति के उच्चतम उत्कर्ष के युग में उत्पन्न हुआ। सबसे पहले यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने, ब्रह्मांड के अर्थ और नियमों को समझने का एक प्रयास था। ग्रीस के प्राचीन दर्शन की शुरुआत, सबसे अधिक संभावना है, मिस्र और एशिया माइनर में होती है - आखिरकार, यहीं पर यूनानियों ने और भी प्राचीन सभ्यताओं के गुप्त ज्ञान के लिए यात्रा की थी।
उल्लेखनीय रूप से, मुख्य दार्शनिक विचार और सिद्धांत ग्रीस के दार्शनिकों द्वारा व्यक्त किए गए थे। नए नामों में व्यावहारिक रूप से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया।
प्राचीन यूनानी दार्शनिकों और उनके अधिक आधुनिक समकक्षों के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे जीवन के बारे में सिर्फ "बात" नहीं करते थे, वे इस तरह से "जीते" थे। दर्शनशास्त्र स्मार्ट पुस्तकों और ग्रंथों में उतना प्रकट नहीं हुआ जितना वास्तविक जीवन में। यदि आपको अपने व्यक्तिगत विश्वासों के लिए कष्ट सहना पड़ा, तो प्राचीन ग्रीस में रहने वाला एक दार्शनिक अपने सिद्धांतों के लिए कष्ट सह सकता था और मर भी सकता था।
प्राचीन यूनानी दर्शन का उदय तब हुआ जब पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें नहीं थीं, उस समय शासक दार्शनिक कहलाना सम्मान की बात समझते थे।
संपूर्ण यूरोपीय और आधुनिक विश्व सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी न किसी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राचीन यूनानी संस्कृति का उत्पाद है।
किसी को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि "प्राचीन ग्रीस" एक सभ्यता को संदर्भित करता है जिसमें बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण में, थ्रेस के तट पर, द्वीपों पर स्थित गुलाम-मालिक राज्य शामिल थे। एजियन समुद्रऔर एशिया माइनर की पश्चिमी तटीय पट्टी पर (VII-VI सदियों)। पहला यूनानी दार्शनिकथेल्स, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमनीज़, पाइथागोरस, ज़ेनोफेनेस, हेराक्लिटस थे। यूनानी दर्शन में तीन कालखंड हैं। पहला: थेल्स से अरस्तू तक। दूसरा: रोमन विश्व में यूनानी दर्शन का विकास। तीसरा: नियोप्लाटोनिक दर्शन। यदि हम कालक्रम को देखें, तो ये तीन कालखंड एक सहस्राब्दी (सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व का अंत - छठी शताब्दी ईस्वी) से अधिक समय को कवर करते हैं।
कुछ शोधकर्ता ग्रीक दर्शन की पहली अवधि को तीन चरणों में विभाजित करते हैं - यह अधिक स्पष्ट रूप से चरित्र और समस्याओं को हल करने में दर्शन के विकास को इंगित करता है। पहला चरण मिलिटस (मिलिटस शहर के नाम से) स्कूल के दार्शनिकों की गतिविधि है: थेल्स, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमनीज़। दूसरा चरण सोफिस्टों, सुकरात और उनके अनुयायियों - सुकरात की गतिविधि है। तीसरा चरण प्लेटो और अरस्तू का दर्शन है। पहले प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की गतिविधि आज तक जीवित नहीं है; इसके बारे में केवल ग्रीस और रोम के बाद के विचारकों और दार्शनिकों के कार्यों से ही सीखा जा सकता है।
विषय पर अधिक:प्राचीन विश्व- ग्रीको-रोमन शास्त्रीय पुरातनता का युग।
- यह एक लगातार विकसित दार्शनिक विचार है, जो 7वीं शताब्दी के अंत से लेकर एक हजार साल से भी अधिक की अवधि को कवर करता है। ईसा पूर्व. छठी शताब्दी तक. विज्ञापन
प्राचीन दर्शन अलगाव में विकसित नहीं हुआ - इसने ऐसे देशों से ज्ञान प्राप्त किया: लीबिया; बेबीलोन; मिस्र; फारस; ; .
इतिहास की दृष्टि से प्राचीन दर्शन को इसमें विभाजित किया गया है:- प्राकृतिक काल(मुख्य ध्यान ब्रह्मांड और प्रकृति पर दिया जाता है - माइल्सियन, एलिया-यू, पाइथागोरस);
- मानवतावादी काल(मुख्य ध्यान मानवीय समस्याओं पर दिया जाता है, सबसे पहले, ये नैतिक समस्याएं हैं; इसमें सुकरात और सोफिस्ट शामिल हैं);
- शास्त्रीय काल(ये प्लेटो और अरस्तू की भव्य दार्शनिक प्रणालियाँ हैं);
- हेलेनिस्टिक स्कूलों की अवधि(मुख्य ध्यान लोगों की नैतिक व्यवस्था पर दिया जाता है - एपिक्यूरियन, स्टोइक, संशयवादी);
- नियोप्लाटोनिज्म(सार्वभौमिक संश्लेषण, एक अच्छे के विचार में लाया गया)।
- प्राचीन दर्शन समधर्मी- इसकी विशेषता बाद के प्रकार के दर्शन की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं का अधिक संलयन, अविभाज्यता है;
- प्राचीन दर्शन ब्रह्मांड केन्द्रित- यह मानव जगत के साथ-साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को भी समाहित करता है;
- प्राचीन दर्शन सर्वेश्वरवादी- यह ब्रह्मांड से आता है, समझदार और कामुक;
- प्राचीन दर्शन शायद ही कानून जानता हो- उसने वैचारिक स्तर पर बहुत कुछ हासिल किया, जिसे पुरातनता का तर्क कहा जाता है सामान्य नामों, अवधारणाओं का तर्क;
- प्राचीन दर्शन की अपनी नैतिकता है - पुरातनता की नैतिकता, पुण्य नैतिकता,कर्तव्य और मूल्यों की बाद की नैतिकता के विपरीत, पुरातनता के युग के दार्शनिकों ने एक व्यक्ति को गुणों और अवगुणों से संपन्न बताया, अपनी नैतिकता के विकास में वे असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच गए;
- प्राचीन दर्शन कार्यात्मक- वह अपने जीवन में लोगों की मदद करना चाहती है, उस युग के दार्शनिकों ने अस्तित्व के प्रमुख सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की।
- इस दर्शन के फलने-फूलने का भौतिक आधार नीतियों का आर्थिक उत्कर्ष था;
- प्राचीन यूनानी दर्शन को भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया से काट दिया गया था, और दार्शनिक एक स्वतंत्र परत में बदल गए, जो शारीरिक श्रम से बोझिल नहीं था;
- प्राचीन यूनानी दर्शन का मूल विचार ब्रह्माण्डकेंद्रितवाद था;
- बाद के चरणों में ब्रह्माण्डकेन्द्रवाद और मानवकेन्द्रवाद का मिश्रण था;
- उन देवताओं के अस्तित्व की अनुमति थी जो प्रकृति का हिस्सा थे और लोगों के करीब थे;
- मनुष्य आसपास की दुनिया से अलग नहीं था, प्रकृति का हिस्सा था;
- दर्शनशास्त्र में दो दिशाएँ निर्धारित की गईं - आदर्शवादीऔर भौतिकवादी.
प्राचीन दर्शन के मुख्य प्रतिनिधि:थेल्स, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमनीज़, पाइथागोरस, इफिसस के हेराक्लिटस, ज़ेनोफेनेस, पारमेनाइड्स, एम्पेडोकल्स, एनाक्सागोरस, प्रोटागोरस, गोर्गियास, प्रोडिकस, एपिकुरस।
प्राचीन दर्शन की समस्याएं: सबसे महत्वपूर्ण के बारे में संक्षेप में
प्राचीन दर्शन बहु-समस्याग्रस्त हैवह खोजबीन करती है विभिन्न समस्याएं: प्राकृतिक-दार्शनिक; ऑन्टोलॉजिकल; ज्ञानमीमांसा; पद्धतिपरक; सौंदर्य संबंधी; पहेली; नैतिक; राजनीतिक; कानूनी।
प्राचीन दर्शन में, ज्ञान को इस प्रकार माना जाता है: अनुभवजन्य; कामुक; तर्कसंगत; तार्किक.
प्राचीन दर्शन में, तर्क की समस्या का विकास किया जा रहा है, इसके अध्ययन में एक महान योगदान दिया गया है, और।
प्राचीन दर्शन में सामाजिक समस्याओं में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है: राज्य और कानून; काम; नियंत्रण; युद्ध और शांति; सत्ता की इच्छाएँ और हित; समाज का संपत्ति विभाजन.
प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार आदर्श शासक में सत्य, सौंदर्य, अच्छाई का ज्ञान जैसे गुण होने चाहिए; बुद्धि, साहस, न्याय, बुद्धि; उसके पास सभी मानवीय क्षमताओं का बुद्धिमानीपूर्ण संतुलन होना चाहिए।
प्राचीन दर्शन था बड़ा प्रभावइसके बाद के दार्शनिक विचार, संस्कृति, मानव सभ्यता के विकास पर।
प्राचीन ग्रीस के पहले दार्शनिक स्कूल और उनके विचार
विचार के पहले, पूर्व-सुकराती स्कूल प्राचीन ग्रीस 7वीं-5वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ। ईसा पूर्व इ। प्रारंभिक प्राचीन यूनानी नीतियां जो गठन की प्रक्रिया में थीं। सबसे प्रसिद्ध को प्रारंभिक दार्शनिक स्कूलनिम्नलिखित पाँच स्कूल शामिल हैं:
माइल्सियन स्कूल
पहले दार्शनिक पूर्व और एशिया (आधुनिक तुर्की का क्षेत्र) की सीमा पर मिलेटस शहर के निवासी थे। माइल्सियन दार्शनिकों (थेल्स, एनाक्सिमनीज़, एनाक्सिमेंडर) ने दुनिया की उत्पत्ति के बारे में पहली परिकल्पना की पुष्टि की।
थेल्स(लगभग 640 - 560 ईसा पूर्व) - माइल्सियन स्कूल के संस्थापक, सबसे पहले प्रमुख यूनानी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों में से एक का मानना था कि दुनिया में पानी है, जिसके द्वारा उन्होंने उस पदार्थ को नहीं समझा जिसे हम देखने के आदी हैं, बल्कि एक निश्चित भौतिक तत्व.
दर्शनशास्त्र में अमूर्त सोच के विकास में बड़ी प्रगति हुई है एनाक्सिमेंडर(610 - 540 ईसा पूर्व), थेल्स के एक छात्र, जिन्होंने "आईपेरॉन" में दुनिया की शुरुआत देखी - एक अनंत और अनिश्चित पदार्थ, एक शाश्वत, अथाह, अनंत पदार्थ जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ समाहित है और जिसमें सब कुछ बदल जाएगा . इसके अलावा, उन्होंने सबसे पहले पदार्थ के संरक्षण का नियम निकाला (वास्तव में, उन्होंने पदार्थ की परमाणु संरचना की खोज की): सभी जीवित चीजें, सभी चीजें सूक्ष्म तत्वों से बनी होती हैं; जीवित जीवों की मृत्यु के बाद, पदार्थों के विनाश के बाद, तत्व बने रहते हैं और नए संयोजनों के परिणामस्वरूप, नई चीजों और जीवित जीवों का निर्माण करते हैं, और मनुष्य की उत्पत्ति के विचार को सबसे पहले सामने रखने वाले भी थे। अन्य जानवरों से विकास का परिणाम (चार्ल्स डार्विन की शिक्षाओं का अनुमान)।
एनाक्सिमनीज़(546 - 526 ईसा पूर्व) - एनाक्सिमेंडर के एक छात्र ने हवा में सभी चीजों की शुरुआत देखी। उन्होंने इस विचार को सामने रखा कि पृथ्वी पर सभी पदार्थ हवा की विभिन्न सांद्रता का परिणाम हैं (हवा, संपीड़ित होकर, पहले पानी में बदल जाती है, फिर गाद में, फिर मिट्टी, पत्थर, आदि में)।
इफिसस के हेराक्लिटस का स्कूल
इस काल में इफिसस शहर यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित था। इस शहर से एक दार्शनिक का जीवन जुड़ा हुआ है हेराक्लीटस(6वीं शताब्दी का दूसरा भाग - 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पहला भाग)। वह एक कुलीन परिवार के व्यक्ति थे जिन्होंने चिंतनशील जीवनशैली के लिए सत्ता छोड़ दी। उन्होंने परिकल्पना की कि दुनिया की शुरुआत आग की तरह हुई थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस मामले में हम उस सामग्री, उस सब्सट्रेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिससे सब कुछ बनाया गया है, बल्कि पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हेराक्लीटस का एकमात्र कार्य जो हमें ज्ञात है उसे कहा जाता है "प्रकृति के बारे में"(हालाँकि, सुकरात से पहले के अन्य दार्शनिकों की तरह)।
हेराक्लीटस न केवल विश्व की एकता की समस्या प्रस्तुत करता है। उनकी शिक्षा में चीजों की विविधता को समझाने का आह्वान किया गया है। सीमाओं की वह व्यवस्था क्या है, जिसके कारण किसी वस्तु में गुणात्मक निश्चितता होती है? क्या जो चीज़ है वही है? क्यों? आज, प्राकृतिक विज्ञान के ज्ञान पर भरोसा करते हुए, हम इस प्रश्न (किसी चीज़ की गुणात्मक निश्चितता की सीमा के बारे में) का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और 2500 साल पहले, ऐसी समस्या उत्पन्न करने के लिए भी, एक व्यक्ति के पास एक अद्भुत दिमाग होना चाहिए।
हेराक्लिटस ने कहा कि युद्ध हर चीज का पिता और हर चीज की मां है। इसके बारे मेंविपरीत सिद्धांतों की परस्पर क्रिया के बारे में। उन्होंने लाक्षणिक ढंग से बात की और समकालीनों ने सोचा कि वह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। एक और प्रसिद्ध रूपक यह प्रसिद्ध कहावत है कि आप एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते। "सब कुछ बहता है, सब कुछ बदलता है!" हेराक्लिटस ने कहा. अत: गठन का स्रोत विपरीत सिद्धांतों का संघर्ष है। इसके बाद, यह एक संपूर्ण सिद्धांत, द्वंद्वात्मकता का आधार बन जाएगा। हेराक्लीटस द्वन्द्ववाद का संस्थापक था।
हेराक्लिटस के कई आलोचक थे। उनके सिद्धांत को उनके समकालीनों का समर्थन नहीं मिला। हेराक्लिटस को न केवल भीड़, बल्कि स्वयं दार्शनिक भी नहीं समझते थे। उनके सबसे आधिकारिक प्रतिद्वंद्वी एलिया के दार्शनिक थे (यदि, निश्चित रूप से, कोई प्राचीन दार्शनिकों के "अधिकार" की बात कर सकता है)।
एलीयन स्कूल
एलीटिक्स- एलेन दार्शनिक स्कूल के प्रतिनिधि जो VI - V सदियों में मौजूद थे। ईसा पूर्व इ। आधुनिक इटली के क्षेत्र में प्राचीन यूनानी शहर एलिया में।
इस सम्प्रदाय के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक दार्शनिक थे ज़ेनोफेनेस(सी. 565 - 473 ईसा पूर्व) और उनके अनुयायी पारमेनीडेस(सातवीं-छठी शताब्दी ईसा पूर्व का अंत) और ज़ेनो(सी. 490 - 430 ईसा पूर्व)। पारमेनाइड्स के दृष्टिकोण से, वे लोग जो हेराक्लीटस के विचारों का समर्थन करते थे, वे "दो सिर वाले खाली दिमाग" थे। हम यहां सोचने के विभिन्न तरीके देखते हैं। हेराक्लिटस ने विरोधाभास की संभावना की अनुमति दी, जबकि पारमेनाइड्स और अरस्तू ने एक प्रकार की सोच पर जोर दिया जो विरोधाभास (बहिष्कृत मध्य का कानून) को बाहर करता है। तर्क में विरोधाभास एक गलती है. पारमेनाइड्स इस तथ्य से आगे बढ़ते हैं कि बहिष्कृत मध्य के कानून के आधार पर विरोधाभास का अस्तित्व सोच में अस्वीकार्य है। विपरीत सिद्धांतों का एक साथ अस्तित्व असंभव है।
पाइथागोरस का स्कूल
पाइथागोरस - प्राचीन यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ के समर्थक और अनुयायी पाइथागोरस(छठी की दूसरी छमाही - 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत) संख्या को हर चीज का मूल कारण माना जाता था (संपूर्ण आसपास की वास्तविकता, जो कुछ भी होता है उसे एक संख्या में घटाया जा सकता है और एक संख्या की मदद से मापा जा सकता है)। उन्होंने एक संख्या के माध्यम से दुनिया की अनुभूति की वकालत की (वे एक संख्या के माध्यम से अनुभूति को कामुक और आदर्शवादी चेतना के बीच मध्यवर्ती मानते थे), इकाई को हर चीज का सबसे छोटा कण मानते थे और "प्रोटो-श्रेणियों" को अलग करने की कोशिश करते थे जो द्वंद्वात्मकता को दर्शाते थे। विश्व की एकता (सम-विषम, हल्का-अँधेरा, सीधा-टेढ़ा, दाएँ-बाएँ, नर-नारी, आदि)।
पाइथागोरस की खूबी यह है कि उन्होंने संख्या सिद्धांत की नींव रखी, अंकगणित के सिद्धांत विकसित किए और कई ज्यामितीय समस्याओं के लिए गणितीय समाधान ढूंढे। उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि यदि किसी संगीत वाद्ययंत्र में तारों की लंबाई एक दूसरे के संबंध में 1:2, 2:3 और 3:4 है, तो आप सप्तक, पांचवें और चौथे जैसे संगीत अंतराल प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन रोमन दार्शनिक बोथियस की कहानी के अनुसार, पाइथागोरस को संख्या की प्रधानता का विचार आया, यह देखते हुए कि विभिन्न आकारों के हथौड़ों के एक साथ प्रहार से सामंजस्यपूर्ण व्यंजन उत्पन्न होते हैं। चूँकि हथौड़ों का वजन मापा जा सकता है, मात्रा (संख्या) दुनिया पर राज करती है। उन्होंने ज्यामिति और खगोल विज्ञान में ऐसे संबंधों की तलाश की। इन "शोध" के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वर्गीय पिंड भी संगीतमय सामंजस्य में हैं।
पाइथागोरस का मानना था कि दुनिया का विकास चक्रीय है और सभी घटनाएं एक निश्चित आवृत्ति ("वापसी") के साथ दोहराई जाती हैं। दूसरे शब्दों में, पाइथागोरस का मानना था कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता है, एक निश्चित अवधि के बाद सभी घटनाएं बिल्कुल दोहराई जाती हैं। उन्होंने रहस्यमय गुणों को संख्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और माना कि संख्याएँ किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक गुणों को भी निर्धारित कर सकती हैं।
एटमिस्ट स्कूल
परमाणुवादी एक भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदाय हैं जिनके दार्शनिक (डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस) " निर्माण सामग्री”, सभी चीज़ों की “पहली ईंट” को सूक्ष्म कण – “परमाणु” माना जाता था। ल्यूसिपस (5वीं शताब्दी ईसा पूर्व) को परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता है। ल्यूसिप्पे के बारे में बहुत कम जानकारी है: वह मिलिटस से आया था और इस शहर से जुड़ी प्राकृतिक-दार्शनिक परंपरा का उत्तराधिकारी था। वह पारमेनाइड्स और ज़ेनो से प्रभावित था। यह तर्क दिया गया है कि ल्यूसिपस एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। शायद इस तरह के निर्णय का आधार यह तथ्य था कि ल्यूसिप्पे के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है। हालाँकि ऐसी राय मौजूद है, फिर भी यह अधिक विश्वसनीय लगता है कि ल्यूसिपस अभी भी एक वास्तविक व्यक्ति है। ल्यूसिपस (लगभग 470 या 370 ईसा पूर्व) के शिष्य और साथी को दर्शनशास्त्र में भौतिकवादी दिशा ("डेमोक्रिटस की पंक्ति") का संस्थापक माना जाता था।
डेमोक्रिटस की शिक्षाओं में निम्नलिखित को प्रतिष्ठित किया जा सकता है बुनियादी प्रावधान:
- संपूर्ण भौतिक संसार परमाणुओं से बना है;
- परमाणु सबसे छोटा कण है, सभी चीज़ों की "पहली ईंट";
- परमाणु अविभाज्य है (इस स्थिति का विज्ञान ने आज ही खंडन किया है);
- परमाणुओं का एक अलग आकार होता है (सबसे छोटे से बड़े तक), एक अलग आकार (गोल, आयताकार, वक्र, "हुक के साथ", आदि);
- परमाणुओं के बीच शून्यता से भरा स्थान है;
- परमाणु सतत गति में हैं;
- परमाणुओं का एक चक्र होता है: चीजें, जीवित जीव मौजूद होते हैं, क्षय होते हैं, जिसके बाद भौतिक संसार के नए जीवित जीव और वस्तुएं इन्हीं परमाणुओं से उत्पन्न होती हैं;
- परमाणुओं को संवेदी अनुभूति द्वारा "देखा" नहीं जा सकता।
इस प्रकार, विशेषणिक विशेषताएं थे: एक स्पष्ट ब्रह्मांडकेंद्रितवाद, आसपास की प्रकृति की घटनाओं को समझाने की समस्या पर बढ़ा हुआ ध्यान, उस मूल की खोज जिसने सभी चीजों को जन्म दिया और दार्शनिक शिक्षाओं की सिद्धांतवादी (गैर-बहस योग्य) प्रकृति। प्राचीन दर्शन के विकास में अगले, शास्त्रीय चरण में स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाएगी।
दुनिया में कई अलग-अलग दर्शन और स्कूल हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक मूल्यों की प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य जीवन के अधिक आवश्यक तरीके का उपदेश देते हैं। हालाँकि, उनमें एक बात समान है - वे सभी मनुष्य द्वारा आविष्कार किए गए हैं। इसीलिए, विचारधारा का अध्ययन शुरू करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि एक दार्शनिक क्या है।
साथ ही, न केवल इस शब्द का अर्थ पता लगाना आवश्यक है, बल्कि उन लोगों को याद करने के लिए अतीत में वापस देखना भी आवश्यक है जो दर्शन के पहले स्कूलों की उत्पत्ति पर खड़े थे। आख़िरकार, केवल इसी तरह से कोई दार्शनिक कौन है के प्रश्न का वास्तविक सार समझ सकता है।
वे लोग जिन्होंने स्वयं को महान चिंतन के लिए समर्पित कर दिया है
इसलिए, हमेशा की तरह, कहानी मुख्य से शुरू होनी चाहिए। ऐसे में दार्शनिक कौन है. दरअसल, भविष्य में, यह शब्द पाठ में बहुत बार दिखाई देगा, जिसका अर्थ है कि इसके अर्थ की स्पष्ट समझ के बिना ऐसा करना असंभव है।
ख़ैर, एक दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जिसने स्वयं को पूरी तरह से अस्तित्व के सार के बारे में सोचने के लिए समर्पित कर दिया है। साथ ही, उनकी मुख्य इच्छा जो हो रहा है उसके सार को समझने की इच्छा है, इसलिए बोलने के लिए, जीवन और मृत्यु के पर्दे के पीछे देखने की इच्छा है। वस्तुतः ऐसे प्रतिबिम्ब बदल जाते हैं आम आदमीएक दार्शनिक में.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह के प्रतिबिंब केवल एक क्षणभंगुर शौक या मनोरंजन नहीं हैं, यह उसके जीवन का अर्थ है या यहां तक कि, यदि आप चाहें, तो एक कॉलिंग है। यही कारण है कि महान दार्शनिकों ने अपना सारा खाली समय उन मुद्दों को सुलझाने में समर्पित कर दिया जो उन्हें परेशान करते थे।
दार्शनिक धाराओं में अंतर
अगला कदम यह महसूस करना है कि सभी दार्शनिक अलग-अलग हैं। दुनिया या चीजों के क्रम का कोई सार्वभौमिक दृष्टिकोण नहीं है। भले ही विचारक एक ही विचार या विश्वदृष्टिकोण का पालन करते हों, उनके निर्णयों में हमेशा मतभेद रहेगा।
यह इस तथ्य के कारण है कि दुनिया पर दार्शनिकों के विचार उन पर निर्भर करते हैं निजी अनुभवऔर तथ्यों का विश्लेषण करने की क्षमता। यही कारण है कि सैकड़ों विभिन्न दार्शनिक धाराओं ने दिन का प्रकाश देखा है। और ये सभी अपने सार में अद्वितीय हैं, जो इस विज्ञान को बहुत बहुमुखी और जानकारीपूर्ण बनाता है।
और फिर भी हर चीज़ की शुरुआत होती है, जिसमें दर्शन भी शामिल है। इसलिए, यह बहुत तर्कसंगत होगा कि हम अपनी आँखें अतीत की ओर मोड़ें और उन लोगों के बारे में बात करें जिन्होंने इस अनुशासन की स्थापना की। अर्थात्, प्राचीन विचारकों के बारे में।

सुकरात - पुरातनता के महान दिमागों में से पहले
आपको उस व्यक्ति से शुरुआत करनी चाहिए जिसे महान विचारकों की दुनिया में एक किंवदंती माना जाता है - सुकरात। उनका जन्म और जीवन 469-399 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में हुआ था। दुर्भाग्य से, इस विद्वान व्यक्ति ने अपने विचारों का रिकॉर्ड नहीं रखा, इसलिए उनकी अधिकांश बातें उनके छात्रों के प्रयासों की बदौलत ही हमारे पास आई हैं।
वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह सोचा कि दार्शनिक क्या होता है। सुकरात का मानना था कि जीवन का अर्थ तभी है जब व्यक्ति इसे सार्थक ढंग से जिए। उन्होंने अपने हमवतन लोगों की नैतिकता को भूलने और अपने ही बुराइयों में फंसने के लिए निंदा की।
अफसोस, सुकरात का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने उनकी शिक्षा को पाखंडी बताया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। उन्होंने सजा के क्रियान्वयन की प्रतीक्षा नहीं की और स्वेच्छा से जहर खा लिया।

प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक
यह प्राचीन ग्रीस है जिसे पश्चिमी दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। इस देश में प्राचीन काल के कई महान मस्तिष्कों का जन्म हुआ। और यद्यपि उनकी कुछ शिक्षाओं को समकालीनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले वैज्ञानिक-दार्शनिक 2.5 हजार साल से भी पहले यहां दिखाई दिए थे।
प्लेटो
सुकरात के सभी शिष्यों में प्लेटो सबसे सफल था। शिक्षक के ज्ञान को आत्मसात करने के बाद, उन्होंने अपने आस-पास की दुनिया और उसके कानूनों का अध्ययन करना जारी रखा। इसके अलावा, लोगों के समर्थन से, उन्होंने एथेंस की महान अकादमी की स्थापना की। यहीं पर उन्होंने युवा छात्रों को दार्शनिक विचारों और अवधारणाओं की मूल बातें सिखाईं।
प्लेटो को यकीन था कि उनकी शिक्षाएँ लोगों को वह ज्ञान दे सकती हैं जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने तर्क दिया कि केवल एक शिक्षित और शांतचित्त व्यक्ति ही एक आदर्श राज्य का निर्माण कर सकता है।
अरस्तू
अरस्तू ने पश्चिमी दर्शन के विकास के लिए बहुत कुछ किया। इस यूनानी ने एथेंस अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और उसके शिक्षकों में से एक स्वयं प्लेटो था। चूँकि अरस्तू विशेष विद्वता से प्रतिष्ठित थे, इसलिए उन्हें जल्द ही प्रबंधक के महल में पढ़ाने के लिए बुलाया गया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, उन्होंने स्वयं सिकंदर महान को शिक्षा दी थी।

रोमन दार्शनिक और विचारक
यूनानी विचारकों के कार्यों ने बहुत प्रभावित किया सांस्कृतिक जीवनरोमन साम्राज्य में. प्लेटो और पाइथागोरस के ग्रंथों से प्रोत्साहित होकर, पहले नवोन्मेषी रोमन दार्शनिक दूसरी शताब्दी की शुरुआत में सामने आने लगे। और यद्यपि उनके अधिकांश सिद्धांत यूनानी सिद्धांतों से मिलते जुलते थे, फिर भी उनकी शिक्षाओं में कुछ अंतर थे। विशेष रूप से, यह इस तथ्य के कारण था कि रोमनों की अपनी अवधारणाएँ थीं कि सर्वोच्च अच्छा क्या है।
मार्क टेरेंस वरो
रोम के पहले दार्शनिकों में से एक वरो थे, जिनका जन्म पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अपने जीवन के दौरान उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समर्पित कई रचनाएँ लिखीं। उन्होंने भी बात रखी दिलचस्प सिद्धांतप्रत्येक राष्ट्र के विकास की चार अवस्थाएँ होती हैं: बचपन, युवावस्था, परिपक्वता और बुढ़ापा।
मार्क ट्यूलियस सिसेरो
यह सबसे प्राचीन रोम में से एक है। सिसरो को इतनी प्रसिद्धि इसलिए मिली क्योंकि वह अंततः ग्रीक आध्यात्मिकता और नागरिकता के रोमन प्रेम को एक साथ जोड़ने में सक्षम हो गए।
आज, दर्शन को एक अमूर्त विज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के मानव जीवन के हिस्से के रूप में स्थान देने वाले पहले लोगों में से एक होने के लिए उन्हें महत्व दिया जाता है। सिसरो लोगों को यह विचार बताने में कामयाब रहे कि अगर वे चाहें तो हर कोई समझ सकता है। विशेष रूप से, इसीलिए उन्होंने इसे पेश किया अपना शब्दकोश, कई दार्शनिक शब्दों का सार समझाते हुए।
दिव्य साम्राज्य के महान दार्शनिक
कई लोग लोकतंत्र के विचार का श्रेय यूनानियों को देते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर पृथ्वीएक महान ऋषि, केवल अपने विश्वास पर भरोसा करते हुए, उसी सिद्धांत को सामने रखने में सक्षम थे। यह वह प्राचीन दार्शनिक है जिसे एशिया का मोती माना जाता है।
कन्फ्यूशियस
चीन को हमेशा बुद्धिमान लोगों का देश माना गया है, लेकिन अन्य सभी के बीच विशेष ध्यानकन्फ्यूशियस को दिया जाना चाहिए। यह महान दार्शनिक 551-479 में रहते थे। ईसा पूर्व इ। और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे. उनके शिक्षण का मुख्य कार्य उच्च नैतिकता और व्यक्तिगत गुणों के सिद्धांतों का प्रचार करना था।

नाम सभी जानते हैं
वर्षों से सब कुछ अधिक लोगदार्शनिक विचारों के विकास में योगदान देना चाहते थे। अधिक से अधिक नए स्कूलों और आंदोलनों का जन्म हुआ और उनके प्रतिनिधियों के बीच जीवंत चर्चा सामान्य आदर्श बन गई। हालाँकि, ऐसी स्थितियों में भी, ऐसे लोग थे जिनके विचार दार्शनिकों की दुनिया के लिए ताज़ी हवा के झोंके की तरह थे।
एविसेना
अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सिना पूरा नामएविसेना, महान का जन्म 980 में फ़ारसी साम्राज्य के क्षेत्र में हुआ था। अपने जीवन के दौरान उन्होंने एक दर्जन से अधिक रचनाएँ लिखीं वैज्ञानिक ग्रंथभौतिकी और दर्शनशास्त्र से सम्बंधित।
इसके अलावा, उन्होंने अपना खुद का स्कूल भी स्थापित किया। इसमें उन्होंने प्रतिभाशाली नवयुवकों को चिकित्सा की शिक्षा दी, जिसमें, वैसे, वे बहुत सफल रहे।

थॉमस एक्विनास
1225 में थॉमस नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। उनके माता-पिता सोच भी नहीं सकते थे कि भविष्य में वह दार्शनिक जगत के सबसे उत्कृष्ट दिमागों में से एक बन जायेंगे। उन्होंने ईसाइयों की दुनिया पर चिंतन के लिए समर्पित कई रचनाएँ लिखीं।
इसके अलावा, 1879 में कैथोलिक चर्चउनके लेखन को मान्यता दी और उन्हें कैथोलिकों के लिए आधिकारिक दर्शन बनाया।
रेने डेस्कर्टेस
उन्हें आधुनिक विचारधारा के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत से लोग उनके जुमले को जानते हैं "अगर मैं सोचता हूं, तो मेरा अस्तित्व है।" अपने कार्यों में उन्होंने मन को मनुष्य का मुख्य हथियार माना। वैज्ञानिक ने विभिन्न युगों के दार्शनिकों के कार्यों का अध्ययन किया और उन्हें अपने समकालीनों तक पहुँचाया।
इसके अलावा, डेसकार्टेस ने अन्य विज्ञानों, विशेष रूप से गणित और भौतिकी में कई नई खोजें कीं।
प्राचीन विश्व के दर्शन को इसमें विभाजित किया गया है:
- - प्राचीन पूर्व का दर्शन
- - प्राचीन दर्शन.
- 1. प्राचीन पूर्व के दर्शन का प्रतिनिधित्व प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, भारत और चीन की संस्कृतियों द्वारा किया जाता है।
प्राचीन मिस्र और बेबीलोन.
पहले दार्शनिक विचारों ने प्राचीन बेबीलोन और प्राचीन मिस्र में आकार लेना शुरू किया, जहां गुलाम-मालिक समाज का गठन 4-3 हजार ईसा पूर्व में हुआ था और इसलिए, कुछ लोगों के लिए मानसिक कार्य में संलग्न होना संभव हो गया।
दार्शनिक विचार की उत्पत्ति दो शक्तिशाली प्रक्रियाओं के प्रभाव में, विषम रूप से आगे बढ़ी:
- - एक ओर - ब्रह्मांड संबंधी पौराणिक कथाएँ
- दूसरी ओर, वैज्ञानिक ज्ञान.
इसका असर उनके चरित्र पर पड़ा.
1. दार्शनिक चिंतन में संसार के भौतिक मूलभूत सिद्धांत के बारे में विचार शामिल थे। इस प्रकार, जल सभी जीवित प्राणियों का स्रोत था।
प्राचीन मिस्र के स्मारकों में अक्सर उस हवा का उल्लेख किया जाता है जो अंतरिक्ष को भरती है और "सभी चीजों में निवास करती है।"
2. प्राचीन मिस्र की "थियोगोनी" और "कॉस्मोगोनी"।
प्रकाशकों, ग्रहों और सितारों को एक बड़ी भूमिका सौंपी गई। उन्होंने न केवल समय की गणना करने और भविष्यवाणियां करने में भूमिका निभाई, बल्कि दुनिया बनाने और उस पर (दुनिया पर) लगातार काम करने वाली शक्तियों के रूप में भी भूमिका निभाई।
3. धार्मिक पौराणिक कथाओं के संबंध में संशयवाद के दर्शन में उत्पत्ति।
लिखित स्मारक:
- - द बुक ऑफ द डेड दुनिया की सबसे पुरानी किताब है।
- - "जीवन के अर्थ के बारे में स्वामी और दास के बीच संवाद"
- - "हार्पर का गीत"
- - "निराश की उसके जज्बे से बातचीत।"
यहां (मिस्र, बेबीलोन) दार्शनिक विचार अभी तक उस समय के अधिक विकसित देशों की विशेषता के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। फिर भी, मिस्रवासियों के विचारों का विज्ञान और दार्शनिक विचार के बाद के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
प्राचीन भारत:
भारत में, दर्शन का उदय हुआ (जैसा कि भारतीय दार्शनिक संस्कृति के स्मारक गवाही देते हैं) दूसरी - पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में, जब उत्तर-पश्चिम से आर्यों (मवेशी-प्रजनन जनजातियों) का आक्रमण हुआ, उनके द्वारा देश की आबादी पर विजय प्राप्त की गई। आदिम साम्प्रदायिक व्यवस्था के विघटन से किसका उदय हुआ प्राचीन भारतवर्ग समाज और राज्य.
प्रथम चरण - वैदिक:
प्राचीन भारतीयों के विचार का पहला स्मारक वेद थे (संस्कृत से अनुवादित का अर्थ है "ज्ञान"), जिसने दर्शन के विकास सहित प्राचीन भारतीय समाज की आध्यात्मिक संस्कृति के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई।
वेदों की रचना, स्पष्ट रूप से, 1500 से 600 ईसा पूर्व में की गई थी, वे धार्मिक भजनों, मंत्रों, शिक्षाओं, प्राकृतिक चक्रों के अवलोकन, उत्पत्ति के बारे में "भोले" विचारों - ब्रह्मांड के निर्माण का एक व्यापक संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वेदों को 4 भागों में बांटा गया है:
- - संहिता - धार्मिक भजन, "पवित्र ग्रंथ";
- - ब्राह्मण - अनुष्ठान ग्रंथों का संग्रह;
- - अराम्याकी - वन साधुओं की पुस्तकें (उनके व्यवहार के नियमों के साथ);
- - उपनिषद (शिक्षक के चरणों में आसन) - वेदों पर दार्शनिक टिप्पणियाँ।
- चरण 2 - महाकाव्य (600 ईसा पूर्व - 200 ईसा पूर्व):
इस समय भारतीय संस्कृति के दो महान महाकाव्यों की रचना हुई - काव्य "रामायण" और "महाभारत"।
* दार्शनिक विद्यालय प्रकट होते हैं, क्योंकि प्राचीन भारतीय दर्शन की विशेषता कुछ प्रणालियों या विद्यालयों के भीतर विकास है।
ये स्कूल दो बड़े समूहों में विभाजित हैं:
- समूह 1: रूढ़िवादी - वेदों के अधिकार को पहचानना।
- 1. सांख्य - छठी शताब्दी ई.पू
- 2. वानज़ेहिश्का - 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व
- 3. मीमांसा - 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व
- 4. वेदांत - 4-2 शताब्दी ईसा पूर्व
- 5. न्याय - तीसरी शताब्दी ई.पू
- 6. योग - द्वितीय शताब्दी ई.पू
- समूह 2: अपरंपरागत (वेदों के अधिकार को नहीं पहचानना)।
- 1. जैन धर्म - चौथी शताब्दी ईसा पूर्व
- 2. बौद्ध धर्म 7-6 शताब्दी ईसा पूर्व
- 3. चार्वाक - लोकायत।
- चरण 3 - सूत्र लेखन (तीसरी शताब्दी ई. - 7वीं शताब्दी ई.):
संचित दार्शनिक सामग्री का व्यवस्थितकरण और सामान्यीकरण होता है।
प्राचीन भारत के दार्शनिक विद्यालयों की सामान्य विशेषताएँ:
- 1. पर्यावरण और व्यक्तित्व का गहरा संबंध है। वी.एल. सोलोविएव (रूसी दार्शनिक): "सब कुछ एक है - यह दर्शन का पहला शब्द था, और इस शब्द ने पहली बार मानव जाति को उसकी स्वतंत्रता और भाईचारे की एकता की घोषणा की ... सब कुछ एक ही सार का संशोधन है।"
- 2. प्राचीन भारत का दर्शन मनुष्य की ओर निर्देशित है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति और आत्मज्ञान और आनंद की स्थिति की प्राप्ति है - निर्वाण।
- 3. जीवन सिद्धांत- तप, आत्मनिरीक्षण, आत्म-गहनता, कर्म नहीं। वे। दर्शन न केवल एक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, बल्कि एक जीवन पद्धति, जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है।
- 4. दर्शनशास्त्र अमूर्त है, यह मूल कारण, निरपेक्ष की समस्याओं को हल करता है, आत्माओं का मालिक क्या है, इस पर प्रतिबिंबित करता है।
- 5. पुनर्जन्म का सिद्धांत - पुनर्जन्म की एक अंतहीन श्रृंखला, जीवन और मृत्यु का शाश्वत चक्र। ब्रह्मांडीय व्यवस्था और समीचीनता का नियम निर्जीव पदार्थ को जीवित पदार्थ में, जीवित पदार्थ को चेतन, तर्कसंगत में और तर्कसंगत पदार्थ को आध्यात्मिक, नैतिक पूर्णता की ओर बदलने का प्रयास करता है।
- 6. कर्म का सिद्धांत - प्रत्येक व्यक्ति के बुरे और अच्छे कर्मों का योग। कर्म ही अगले जन्म का स्वरूप निर्धारित करता है।
वह। भारतीय दर्शन भौतिक जगत पर पूर्ण निर्भरता से उसकी स्वतंत्रता की ओर मानवीय आत्मा की एक बड़ी छलांग थी।
बी. प्राचीन चीन.
चीन प्राचीन इतिहास, संस्कृति और दर्शन का देश है। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में, शान-यिन (18-12 शताब्दी ईसा पूर्व) राज्य में, एक दास-स्वामी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ।
12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, युद्ध के परिणामस्वरूप, झोउ जनजाति द्वारा शान-यिन राज्य को नष्ट कर दिया गया, जिसने अपना राजवंश बनाया।
221 ईसा पूर्व में, चीन शक्तिशाली किन साम्राज्य में एकजुट हुआ और शुरू हुआ नया मंचराज्य और दर्शन का विकास।
चीन का दर्शन कई सार्वभौमिक समस्याओं का समाधान करता है:
- - प्रकृति, समाज, मनुष्य के प्रति जागरूकता
- - मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध.
प्राचीन चीन में मुख्य दार्शनिक विद्यालय:
- 1. प्राकृतिक दार्शनिकों (यिन और यांग के सिद्धांत के समर्थक) ने विपरीत सिद्धांतों (पुरुष और महिला, अंधेरा और प्रकाश, सूर्योदय और सूर्यास्त) का सिद्धांत विकसित किया। सिद्धांतों के बीच सामंजस्य, सहमति खोजना - यह उस समय के दर्शन के कार्यों में से एक है।
- 2. कन्फ्यूशीवाद (कन्फ्यूशियस 551-479 ईसा पूर्व - सबसे प्रमुख विचारक और राजनीतिज्ञ, कन्फ्यूशियस स्कूल के संस्थापक):
- *कन्फ्यूशियस के विचार स्वर्ग की पारंपरिक धार्मिक अवधारणा पर आधारित थे। यह एक महान शुरुआत है, सर्वोच्च देवता, जो मनुष्य को अपनी इच्छा निर्देशित करता है। आकाश सार्वभौमिक पूर्वज और महान शासक है: यह मानव जाति को जन्म देता है और उसे जीवन के नियम देता है।
- * पुरातनता का आदर्शीकरण, पूर्वजों का पंथ, एसएनएफ के मानदंडों को पूरा करना - माता-पिता के लिए सम्मान और देखभाल के पुत्र।
- * प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नियुक्ति के अनुरूप होना चाहिए और आज्ञाकारी होना चाहिए (अधीनस्थता के अनुसार)
- 3. ताओवाद - महान ताओ का सिद्धांत (चीजों के तरीके के बारे में)।
लाओ त्ज़ु के संस्थापक (6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व)।
मुख्य विचार:
* प्रकृति और लोगों का जीवन "स्वर्ग की इच्छा" से नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित मार्ग-ताओ पर आगे बढ़ता है।
ताओ स्वयं चीजों का प्राकृतिक नियम है, जो त्सी (वायु, ईथर) पदार्थ के साथ मिलकर दुनिया का आधार बनाता है।
*दुनिया में हर चीज़ गतिमान और परिवर्तनशील है, हर चीज़ लगातार बदल रही है, चाहे यह विकास कैसा भी हो, न्याय की जीत होगी। यही कानून है. एक व्यक्ति को चीजों के प्राकृतिक क्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात्। जीवन की सार्थकता स्वाभाविकता एवं अकर्मण्यता का पालन करने में है। आसपास का समाज मनुष्य के लिए हानिकारक है। हमें अपने आसपास के समाज से प्रयास करने की जरूरत है।
चीनी दर्शन की विशेषताएं.
- 1. इसका पौराणिक कथाओं से गहरा संबंध है, लेकिन पौराणिक कथाओं के साथ संबंध सबसे पहले, पिछले राजवंशों, "स्वर्ण युग" के बारे में ऐतिहासिक किंवदंतियों के रूप में प्रकट होता है।
- 2. यह एक तीव्र सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष से जुड़ा है। कई दार्शनिक महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर रहे हैं।
- 3. उसने शायद ही कभी प्राकृतिक विज्ञान सामग्री का सहारा लिया (मॉइस्ट स्कूल इसका अपवाद है)
- 4. सैद्धांतिक खोजों की व्यावहारिकता: व्यक्ति, सरकार का आत्म-सुधार। चीनियों के बीच किसी भी व्यवसाय में नैतिक मानदंड मुख्य सामग्री थे।
- 5. कन्फ्यूशीवाद के संतीकरण ने प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन के बीच एक वैचारिक कानून स्थापित किया।
- 6. चीनी दर्शन को तर्क और प्राकृतिक विज्ञान से अलग करने से वैचारिक तंत्र का निर्माण धीमा हो गया, इसलिए प्राकृतिक-दार्शनिक और वैचारिक प्रकृति का सिद्धांत बनाना दुर्लभ था। अधिकांश चीनी स्कूलों के लिए दार्शनिक विश्लेषण की पद्धति वस्तुतः अज्ञात रही।
- 7. विश्व को एक एकल जीव मानना। दुनिया एक है, इसके सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और सामंजस्यपूर्ण रूप से संतुलन बनाए रखते हैं।
- 8. पुरातनता का चीनी दर्शन मानवकेंद्रित है, जिसका उद्देश्य सांसारिक ज्ञान की समस्याओं को हल करना है, चीजों के प्राकृतिक पाठ्यक्रम, गैर-क्रिया के प्रति दृष्टिकोण है।
सामान्य तौर पर, प्राचीन पूर्व के दर्शन पर निष्कर्ष।
- 1. इसमें लोगों के विकास की ख़ासियत, उनकी सामाजिक-आर्थिक और राज्य परंपराओं को दर्शाने वाली कई विशेषताएं थीं।
- 2. इस दर्शन के कई सिद्धांत बाद की दार्शनिक प्रणालियों में शामिल किए गए:
- - भारतीय - "अर्थात, आप (या सब कुछ एक है)", - जो कुछ भी मौजूद है उसकी एकता के बारे में दर्शन का पहला शब्द वीएल की एकता के तत्वमीमांसा में परिलक्षित हुआ था। सोलोविएव;
- - मिस्र - भौतिक मूलभूत सिद्धांत के बारे में प्राकृतिक घटनाएंभौतिकवादियों के प्राचीन दर्शन में इसकी झलक मिलती है।
- - चीनी - ए) सभी चीजों के प्राकृतिक मार्ग के बारे में ताओ का दर्शन - ताओ - कांट की नैतिक स्पष्ट अनिवार्यता, हेगेल की द्वंद्वात्मकता में परिलक्षित होता है।
- बी) कन्फ्यूशियस स्कूल आधिकारिक शक्ति को प्रमाणित करने वाला पहला हठधर्मी स्कूल बन गया - यह सोवियत दर्शन में परिलक्षित हुआ।
- 3. अध्ययन किए गए क्षेत्रों में, संस्कृति की अवधि विकसित नहीं हुई - पुनर्जागरण, ज्ञानोदय, सुधार।
- 2. प्राचीन दर्शन के उद्भव का इतिहास
यह ज्ञात है कि हमारी सभ्यता पुरातनता की संतान है, इसलिए प्राचीन दर्शन आधुनिक दर्शन के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है।
प्राचीन दर्शन प्राचीन यूनानियों और प्राचीन रोमनों का दर्शन है।
यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक अस्तित्व में था, यानी। लगभग 1200 वर्ष:
1. शुरुआत - थेल्स (625 - 547 ईसा पूर्व) - अंत - एथेंस में दार्शनिक स्कूलों को बंद करने पर सम्राट जस्टिनियन का फरमान (529 ईस्वी)।
आयोनियन और इतालवी तटों (मिलिटस, इफिसस, एलिया) पर पुरातन नीतियों के निर्माण से लेकर लोकतांत्रिक एथेंस के उत्कर्ष और उसके बाद के संकट और नीति के पतन तक।
दार्शनिक चिंतन का उदय निम्न कारणों से हुआ:
- - समाज की लोकतांत्रिक संरचना;
- - पूर्वी अत्याचार की अनुपस्थिति;
- - सुदूर भौगोलिक स्थिति.
अपने विकास में, प्राचीन दर्शन 4 चरणों से गुज़रा:
चरण 1: 7-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व-सुकराती (19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जर्मन शास्त्रीय भाषाशास्त्री: हरमन डायल्स, वाल्टर क्रांस ने प्राकृतिक दार्शनिक विद्यालयों के सामूहिक पदनाम के लिए "पूर्व-सुकराती" शब्द का परिचय दिया)।
स्कूलों का आयोनियन समूह:
- - माइल्सियन: थेल्स, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमनीज़ (छठी शताब्दी ईसा पूर्व)।
- - एलीटिक स्कूल (5वीं शताब्दी ईसा पूर्व): पारमेनाइड्स, ज़ेनोफेनेस।
- - इफिसुस के हेराक्लीटस.
एथेंस ग्रुप ऑफ़ स्कूल्स:
- - पाइथागोरस और पाइथागोरस।
- - तंत्र और परमाणुवाद: एम्पेडोकल्स, एनाक्सागोरस, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस।
- - सोफिज़्म (5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दूसरा भाग): प्रोटागोरस, गोर्गियास, प्रोडिकस, हिप्पियास।
- चरण 2: शास्त्रीय (5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आधे भाग से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक)।
सुकरात (469 - 399 ईसा पूर्व)।
प्लेटो (427 - 347 ईसा पूर्व)।
अरस्तू (384 - 322 ईसा पूर्व)।
नैतिक विद्यालय:
- - हेडोनिक (अरिस्टिपस)
- - निंदक (विरोधी)।
- चरण 3: हेलेनिस्टिक (चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में)।
दार्शनिक विद्यालय:
- - पेरिपेटेटिक्स (अरस्तू का स्कूल)
- - अकादमिक दर्शन (प्लेटोनिक अकादमी)
- - स्टोइक स्कूल (किशन से ज़ेनो)
- - एपिक्यूरियन (एपिकुरस)
- - संशयवाद।
- चरण 4: रोमन (पहली शताब्दी ईसा पूर्व - 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी)
- - स्टोकिज्म (सेनेका, एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस)
- - एपिक्यूरियनिज़्म (टाइटस ल्यूक्रेटियस कार)
- - संशयवाद (सेक्स्ट एम्पिरिक)।
चरणों की विशेषताएँ.
- प्रथम चरण को प्राकृतिक दर्शन (प्रकृति का दर्शन) के रूप में जाना जाता है।
- 1. यूनानियों के लिए मानव मन की सबसे महत्वपूर्ण खोज कानून (लोगो) है, जिसका हर कोई पालन करता है, और जो एक नागरिक को एक बर्बर से अलग करता है।
- 1. शुरुआत (पहली ईंट) की तलाश है जिससे जो कुछ भी मौजूद है वह बनाया गया है।
- a) एक विशिष्ट पदार्थ से (625-547 ईसा पूर्व)
- * थेल्स के लिए, शुरुआत पानी है (हर चीज़ पानी से आती है और हवा में बदल जाती है)।
- * एनाक्सिमनीज़ (585-525 ईसा पूर्व) में हवा है (इसकी अनंतता और गतिशीलता के कारण), इससे चीजें पैदा होती हैं: "जब डिस्चार्ज किया जाता है, तो आग पैदा होती है, और जब गाढ़ा हो जाता है, तो हवा, फिर कोहरा, पानी, पृथ्वी, पत्थर। और उसी से बाकी सब कुछ आता है।”
- * हेराक्लिटस में आग है। "इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, लेकिन यह हमेशा से एक जीवित अग्नि रही है, है और रहेगी जो विपरीत आकांक्षाओं से अस्तित्व का निर्माण करती है।" आत्मा अग्नि है.
- बी) किसी अनिश्चित चीज़ से
- * एनाक्सिमेंडर (610-545 ईसा पूर्व) में - एपिरॉन (अनंत), "एपिरॉन पदार्थ से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें विपरीत, जैसे कि, जुड़े हुए हैं (गर्म - ठंडा, आदि), जिसका चयन और सभी विकास का कारण बनता है विभिन्न रूपों में. चीज़ों की यह गति शाश्वत है।”
- * ल्यूसिपस (500-440 ईसा पूर्व) और डेमोक्रिटस (460-370 ईसा पूर्व) में एक परमाणु होता है। परमाणु वे तत्व हैं जिनसे संपूर्ण प्रकृति का निर्माण होता है। परमाणु अविभाज्य, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, अभेद्य है। अतः संसार अनादि, अविनाशी है।
परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं:
- - आकार (त्रिकोण, हुक, आदि) में, मानव आत्मा और विचार परमाणुओं से बने होते हैं - गोल, चिकने, छोटे और मोबाइल। वे शरीर में स्थित हैं.
- - आकार (और वजन) में.
- - इस कदम पर।
- ग) चीजों का सार संख्याओं में है।
- * पाइथागोरस (580-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध) - सब कुछ एक संख्या है। पाइथागोरस की संख्या एक अमूर्त मात्रा नहीं है, बल्कि सर्वोच्च इकाई का एक आवश्यक और सक्रिय गुण है, अर्थात। ईश्वर, विश्व सद्भाव का स्रोत। उनकी राय में, संख्याएँ एक निश्चित क्रम, आसपास की दुनिया के सामंजस्य और चीजों और घटनाओं की विविधता को व्यक्त करती हैं। "जहाँ कोई संख्या और माप नहीं है, वहाँ अराजकता और चिमेरा है।"
- घ) चीजों का सार उनके अस्तित्व में है
- * पारमेनाइड्स में - पदार्थ - जैसा होना। “होना है, गैर-अस्तित्व नहीं है, क्योंकि गैर-अस्तित्व को जानना असंभव है (क्योंकि यह समझ से परे है), न ही व्यक्त करना। सत्ता शाश्वत, एक, गतिहीन, अविनाशी, एकरूप और सदैव अपने समान है। यह सजातीय एवं सतत, गोलाकार है। कोई खाली जगह नहीं है - सब कुछ अस्तित्व से भरा हुआ है।
- 2. विश्व की संरचना के ब्रह्माण्ड संबंधी सिद्धांत प्रमाणित हैं।
दुनिया के पदार्थ (या पहली ईंट) की समझ के आधार पर, प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक दुनिया (ब्रह्मांड) की संरचना के अपने स्वयं के ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत बनाते हैं।
- * थेल्स - पृथ्वी पानी की सतह पर तैरती एक सपाट डिस्क है - यह ब्रह्मांड का केंद्र है। तारे, सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी से मिलकर बने हैं और पानी के वाष्पीकरण पर निर्भर हैं, फिर बारिश के दौरान पानी वापस लौट आता है और पृथ्वी में चला जाता है।
- * हेराक्लीटस (प्रथम द्वन्द्ववादी) - उनका ब्रह्माण्ड विज्ञान तात्विक द्वन्द्ववाद पर आधारित है।
विश्व एक व्यवस्थित ब्रह्मांड है। इस ब्रह्माण्ड का निर्माण सामान्य परिवर्तनशीलता, वस्तुओं की तरलता के आधार पर होता है। "सबकुछ बहता है, सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थिर नहीं है"
सारी प्रकृति बिना रुके अपनी स्थिति बदलती रहती है। "आप एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते"
संसार जन्मता है और मरता है।
पूरे आंदोलन के केंद्र में विरोधों का संघर्ष है - यह निरपेक्ष है।
डेमोक्रिटस: परमाणु बेतरतीब ढंग से चलते हैं, टकराते हैं, वे बवंडर बनाते हैं, जिनमें से - पृथ्वी और प्रकाशमान, और बाद में पूरी दुनिया। यह विचार ब्रह्मांड में अनंत संसारों के बारे में है।
स्टेज 2 (क्लासिक) को मानवशास्त्रीय के रूप में जाना जाता है, अर्थात। केन्द्रीय समस्या मनुष्य की समस्या है।
- 1. प्रकृति के प्रमुख अध्ययन से मनुष्य, उसके जीवन की सभी विविध अभिव्यक्तियों पर विचार करने की ओर एक संक्रमण होता है, दर्शन में एक व्यक्तिपरक-मानवशास्त्रीय प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।
- 2. समस्याओं का समाधान होता है:
- ए) किसी व्यक्ति की समस्या, अन्य लोगों के साथ उसके संबंधों का ज्ञान।
सुकरात ने पहली बार मनुष्य की समस्या को एक नैतिक प्राणी के रूप में दर्शन के केंद्र में देखा:
- - मानव नैतिकता की प्रकृति का पता चलता है;
- - परिभाषित करता है कि अच्छाई, बुराई, न्याय, प्रेम, यानी क्या है। मानव आत्मा का सार क्या है;
- - दर्शाता है कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति के रूप में स्वयं के ज्ञान के लिए प्रयास करना आवश्यक है, अर्थात। नैतिक, सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व।
अनुभूति व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य और क्षमता है, क्योंकि अनुभूति की प्रक्रिया के अंत में, हम वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक रूप से मान्य सत्य, अच्छाई, सौंदर्य, अच्छाई और मानवीय खुशी के ज्ञान तक पहुंचते हैं। सुकरात के व्यक्तित्व में मानव मस्तिष्क ने सबसे पहले तार्किक रूप से सोचना शुरू किया।
- बी) राजनीति और राज्य की समस्या और मनुष्य से उनका संबंध।
- * सुकरात - जिस तरह से नागरिक कानूनों को क्रियान्वित करते हैं, उसमें राज्य मजबूत है - प्रत्येक पितृभूमि के लिए और कानून पिता और माता से अधिक ऊंचे और प्रिय होने चाहिए।
- * प्लेटो - ने "आदर्श राज्य" का सिद्धांत बनाया, जिससे समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया:
- प्रथम - प्रबंधक - दार्शनिक
- दूसरा - रक्षक (योद्धा)
- तीसरा - निचला (किसान, कारीगर, व्यापारी)।
- - राज्य विचारों का अवतार है, और लोग खिलौनों की तरह कार्य करते हैं, जिनका आविष्कार और नियंत्रण ईश्वर द्वारा किया जाता है।
- * अरस्तू - एक व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, दूसरे के लिए चिंता की अभिव्यक्ति समाज के लिए चिंता की अभिव्यक्ति है।
- सी) संश्लेषण की समस्याएं दार्शनिक ज्ञान, आध्यात्मिक प्रणालियों का निर्माण जो दो दुनियाओं को पहचानती है - विचारों की दुनिया और तरल, चीजों की मोबाइल दुनिया, इन दुनियाओं को जानने की तर्कसंगत विधि की खोज।
- *प्लेटो आदर्शवादी यूरोपीय दर्शन के संस्थापक हैं।
- 1. पहली बार, उन्होंने सच्चे अस्तित्व की प्रकृति (भौतिकवादियों और आदर्शवादियों पर) के प्रश्न के समाधान के आधार पर, दर्शन को दो धाराओं में विभाजित किया।
- 2. प्लेटो ने अतीन्द्रिय अस्तित्व के क्षेत्र की खोज की - "विचारों की दुनिया"। मूल सिद्धांत विचारों की दुनिया है। विचारों को महसूस नहीं किया जा सकता, उन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। विचारों पर केवल मन द्वारा, अवधारणाओं के माध्यम से "चिंतन" किया जा सकता है। भौतिक संसार भी आवश्यक है, परंतु वह विचारों के संसार की छाया मात्र है। सच्चा अस्तित्व विचारों का संसार है। प्लेटो ने विचारों की दुनिया को एक दिव्य क्षेत्र घोषित किया, जिसमें व्यक्ति के जन्म से पहले उसकी अमर आत्मा निवास करती है। फिर वह पापी पृथ्वी पर पहुँचती है और अस्थायी रूप से मानव शरीर में रहते हुए, विचारों की दुनिया को याद करती है।
इस प्रकार, ज्ञान आत्मा द्वारा अपने पूर्व-पृथ्वी अस्तित्व की स्मृति है।
*अरस्तू प्लेटो का शिष्य है, उसकी रचनाएँ शिखर पर मानी जाती हैं
प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक विचार.
उनकी शिक्षाओं के मुख्य प्रावधान:
- - विचारों के प्लेटोनिक सिद्धांत की आलोचना की ("प्लेटो मेरा मित्र है, लेकिन सत्य अधिक प्रिय है");
- - श्रेणियों (सार और गुणवत्ता) का सिद्धांत बनाया;
- - पदार्थ और रूप का सिद्धांत: वह पदार्थ की अवधारणा को पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इसे शाश्वत, अनुपचारित, अविनाशी के रूप में पहचाना;
- - विज्ञान के बीच सैद्धांतिक, व्यावहारिक और रचनात्मक में अंतर किया गया:
सैद्धांतिक:
- - तत्वमीमांसा (या वास्तव में दर्शन) - सभी चीजों के मूल कारणों, सभी चीजों की उत्पत्ति का अध्ययन करता है;
- - भौतिकी - निकायों की स्थिति और कुछ "पदार्थ" का अध्ययन करता है;
- - गणित - वास्तविक चीज़ों के अमूर्त गुण।
व्यावहारिक:
- - नैतिकता - व्यवहार के आदर्श का विज्ञान
- - अर्थशास्त्र, राजनीति
रचनात्मक:
- - काव्यशास्त्र
- - बयानबाजी.
- - तर्क का विज्ञान विकसित किया, इसे अस्तित्व के अध्ययन के लिए "जैविक" विज्ञान कहा, इसमें अनुभूति की एक विधि - प्रेरण की पहचान की;
- - आत्मा का सिद्धांत, जिस पर अरिस्टोटेलियन नैतिकता आधारित है।
- तीसरा चरण: हेलेनिस्टिक।
प्राचीन यूनानी दास समाज के पतन से जुड़ा, ग्रीस का पतन। इस संकट के कारण एथेंस और अन्य यूनानी नीतियों के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता का ह्रास हुआ। एथेंस सिकंदर महान द्वारा बनाई गई विशाल शक्ति का हिस्सा बन गया।
विजेता की मृत्यु के बाद राज्य के पतन ने संकट के विकास को तेज कर दिया, जिससे समाज के आध्यात्मिक जीवन में गहरा परिवर्तन हुआ।
इस चरण के दर्शन की सामान्य विशेषताएँ:
प्लेटो और अरस्तू की शिक्षाओं पर टिप्पणी करने से लेकर नैतिकता की समस्याओं, संशयवाद और रूढ़िवाद का प्रचार करने तक का संक्रमण:
संशयवाद एक दार्शनिक अवधारणा है जो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को जानने की संभावना पर सवाल उठाती है।
Stoicism एक सिद्धांत है जो जीवन के आदर्श - समता और शांति, आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया न करने की क्षमता की घोषणा करता है।
मुख्य समस्याएँ:
- - नैतिकता और मानव स्वतंत्रता, खुशी की उपलब्धि;
- - दुनिया को जानने की संभावना की समस्याएं;
- - ब्रह्मांड की संरचनाएं, ब्रह्मांड और मनुष्य का भाग्य;
- - भगवान और मनुष्य के बीच संबंध.
- चौथा चरण: रोमन
इस अवधि के दौरान, रोम ने प्राचीन विश्व में एक निर्णायक भूमिका निभानी शुरू कर दी, जिसके प्रभाव में ग्रीस आ गया। रोमन दर्शन का निर्माण ग्रीक, विशेषकर हेलेनिस्टिक काल के प्रभाव में हुआ है। वे। यह Stoicism और Epicureanism विकसित करता है, जो अपनी विशेषताओं को प्राप्त करते हैं।
रोमन साम्राज्य के पतन के दौरान, समाज का संकट गहरा गया, जिसके कारण व्यक्तिगत अस्तित्व का विनाश हुआ।
धर्म और रहस्यवाद के प्रति बढ़ती लालसा।
उस समय के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, दर्शन स्वयं एक धर्म बन गया, ईसाई धर्म के लिए एक पुल।
- 1. प्राचीन दर्शन वस्तुवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि विषय अभी वस्तु से ऊंचा नहीं हुआ है (जैसा कि नए यूरोपीय दर्शन में हुआ)।
- 2. प्राचीन दर्शन कामुक ब्रह्मांड से आगे बढ़ता है, न कि पूर्ण व्यक्तित्व से (जो मध्य युग की विशेषता है)।
- 3. ब्रह्मांड एक पूर्ण देवता है, जिसका अर्थ है कि प्राचीन दर्शन सर्वेश्वरवादी है, अर्थात। ईश्वर और प्रकृति की पहचान कराता है। ग्रीक देवताओंप्राकृतिक और मानव जैसा। अंतरिक्ष एनिमेटेड है.
- 4. स्थान आवश्यकता का कारण बनता है। मनुष्य के संबंध में आवश्यकता ही भाग्य है। लेकिन चूँकि वह उसे निश्चित रूप से नहीं जानती, इसलिए वह कोई विकल्प चुन सकता है।
- 5. प्राचीन दर्शन अवधारणाओं (श्रेणियों) के विकास में उच्च स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन यह लगभग कोई कानून नहीं जानता है।
- 6. प्राचीन दर्शन में अभी भी भौतिकवाद और आदर्शवाद के बीच कोई स्पष्ट विरोध नहीं है और दोनों दिशाएँ सहज हैं।
- 3. मध्यकालीन दर्शन
दर्शन मध्य युग प्राचीन आदर्शवाद
मध्यकालीन यूरोपीय दर्शन दर्शन के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्थक एवं लम्बा चरण है।
कालानुक्रमिक रूप से, यह अवधि 5वीं - 15वीं शताब्दी को कवर करती है।
इस काल की विशेषताएँ:
- 1. सामंतवाद के युग का निर्माण एवं उत्कर्ष।
- 2. जनमानस में धर्म एवं चर्च का प्रभुत्व। ईसाई धर्म राज्य धर्म बन गया। एफ. एंगेल्स: "चर्च की हठधर्मिता एक ही समय में राजनीतिक सिद्धांत बन गई, और बाइबिल के ग्रंथों को हर अदालत में कानून का बल प्राप्त हुआ।"
- 3. चर्च ने शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान के विकास की सभी प्रक्रियाओं पर एकाधिकार कर लिया है।
अधिकांश वैज्ञानिक पादरी वर्ग के प्रतिनिधि थे, और मठ संस्कृति और विज्ञान के केंद्र थे।
इसने मध्य युग के दर्शन की प्रकृति को निर्धारित किया:
- - दार्शनिक विचार का आंदोलन धर्म की समस्याओं से व्याप्त था;
- - चर्च हठधर्मिता प्रारंभिक बिंदु और आधार थी दार्शनिक सोच;
- - दर्शनशास्त्र अक्सर धार्मिक वैचारिक तंत्र का उपयोग करता है;
- - किसी भी दार्शनिक अवधारणा को, एक नियम के रूप में, चर्च की शिक्षाओं के अनुरूप लाया गया था;
- - दर्शन सचेतन रूप से स्वयं को धर्म की सेवा में लगाता है "दर्शन धर्मशास्त्र का सेवक है।"
मध्यकालीन दर्शन में दो प्रवृत्तियाँ:
- पहला - पवित्रीकरण - धार्मिक शिक्षाओं के साथ मेल-मिलाप;
- दूसरा - नैतिकता - नैतिकता के साथ तालमेल, यानी। व्यावहारिक अभिविन्यासविश्व में ईसाई व्यवहार के नियमों को प्रमाणित करने वाला दर्शन।
मध्यकालीन दर्शन की विशेषताएं.
1. थियोसेंट्रिकिटी - यानी सर्वोच्च वास्तविकता प्रकृति नहीं, बल्कि ईश्वर है।
विश्वदृष्टि के मुख्य सिद्धांत:
- ए) सृजनवाद (या सृजन) - अर्थात। ईश्वर द्वारा शून्य से संसार की रचना का सिद्धांत।
- - ईश्वर शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है, वह सभी अस्तित्वों का स्रोत है और ज्ञान के लिए दुर्गम है। ईश्वर सर्वोच्च अच्छा है।
- - संसार परिवर्तनशील, नश्वर, क्षणभंगुर, परिपूर्ण और अच्छा है क्योंकि यह ईश्वर द्वारा बनाया गया है।
- बी) रहस्योद्घाटन का सिद्धांत - सैद्धांतिक रूप से नश्वर लोगों के लिए अनुभूति के लिए दुर्गम होने के कारण, ईसाई भगवान ने खुद को रहस्योद्घाटन के माध्यम से प्रकट किया, जो पवित्र पुस्तकों - बाइबिल में दर्ज है। मानव आत्मा की एक विशेष क्षमता के रूप में ज्ञान का मुख्य साधन विश्वास था।
धर्मशास्त्री-दार्शनिक का कार्य बाइबिल ग्रंथों के रहस्यों और रहस्यों को उजागर करना है और इस प्रकार उच्च वास्तविकता के ज्ञान तक पहुंचना है।
- 2. पूर्वव्यापीता - मध्ययुगीन दर्शन को अतीत की ओर मोड़ दिया गया है, क्योंकि मध्ययुगीन चेतना की कहावत कहती है: "जितना पुराना, उतना अधिक प्रामाणिक, उतना ही अधिक प्रामाणिक, उतना ही अधिक ईमानदार" (और सबसे प्राचीन दस्तावेज़ बाइबिल था)।
- 3. परंपरावाद - एक मध्ययुगीन दार्शनिक के लिए, किसी भी प्रकार के नवाचार को गौरव का प्रतीक माना जाता था, उसे लगातार स्थापित मॉडल, कैनन का पालन करना पड़ता था। दार्शनिक की राय का दूसरों की राय से मेल खाना उसके विचारों की सत्यता का सूचक था।
- 4. उपदेशवाद (शिक्षण, संपादन) - मुक्ति के दृष्टिकोण से, ईश्वर की ओर शिक्षा और पालन-पोषण के मूल्य पर स्थापना। दार्शनिक ग्रंथों का रूप एक आधिकारिक शिक्षक और एक विनम्र सहमति देने वाले छात्र के बीच का संवाद है।
शिक्षक गुण:
- - पवित्र शास्त्रों का गुणी ज्ञान
- - अरस्तू के औपचारिक तर्क के नियमों का ज्ञान.
मध्यकालीन दर्शन के चरण.
दर्शन के इतिहास में चरण 1-पैट्रिस्टिक्स (शब्द "पेटर" से - पिता, जिसका अर्थ है "चर्च का पिता") पहली-छठी शताब्दी से निर्धारित होता है।
देशभक्तों के शिखर पर ऑगस्टीन द धन्य (354-430) हैं, जिनके विचारों ने यूरोपीय दर्शन के विकास को निर्धारित किया।
स्टेज विशेषताएँ:
- - ईसाई हठधर्मिता और दर्शन का बौद्धिक डिजाइन और विकास;
- - प्लैटोनिज्म के दार्शनिक तत्व निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
देशभक्तों की मुख्य समस्याएँ:
- 1. ईश्वर के सार और उसकी त्रिमूर्ति (त्रिमूर्ति समस्या) की समस्या।
- 2. विश्वास और तर्क का संबंध, ईसाइयों का रहस्योद्घाटन और बुतपरस्तों (यूनानी और रोमन) का ज्ञान।
- 3. इतिहास को एक निश्चित अंतिम लक्ष्य की ओर एक आंदोलन के रूप में समझना और इस लक्ष्य की परिभाषा - "भगवान का शहर"।
- 4. अपनी आत्मा की मुक्ति या मृत्यु की संभावना के माध्यम से मानव स्वतंत्रता का दृष्टिकोण।
- 5. संसार में बुराई की उत्पत्ति की समस्या, और ईश्वर इसे क्यों सहन करता है।
- दूसरा चरण - स्कोलास्टिज्म (9वीं-15वीं शताब्दी, ग्रीक स्कोला - स्कूल से) - दर्शन का एक रूप व्यापक रूप से स्कूलों में और फिर पश्चिमी यूरोप के विश्वविद्यालयों में (12वीं शताब्दी से) पढ़ाया जाता है।
थॉमस एक्विनास (1223-1274) - मध्ययुगीन विद्वतावाद के शिखर, सभी उत्तर-प्राचीन दर्शन के महानतम दार्शनिकों में से एक।
स्टेज विशेषताएँ:
- 1. ईसाई दर्शन का व्यवस्थितकरण (1323 में थॉमस एक्विनास को होली सी द्वारा संत घोषित किया गया था, और उनकी प्रणाली रोमन कैथोलिक चर्च का आधिकारिक दार्शनिक सिद्धांत बन गई)।
- 2. अरस्तू की दार्शनिक शिक्षा ईसाई दर्शन के व्यवस्थितकरण में निर्णायक भूमिका निभाती है।
विद्वतावाद की मुख्य समस्याएँ:
1. धर्म, दर्शन, विज्ञान का सहसंबंध। एक ऐसे विज्ञान के रूप में दर्शनशास्त्र की ओर ध्यान बढ़ रहा है जो पूरी तरह से धर्म के अनुकूल है और मानव आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचता है। प्राचीन दर्शन अब धर्म का शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धी नहीं रहा।
- - इस पर अधिक ध्यान, इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार;
- - और सबसे महत्वपूर्ण बात - धार्मिक समस्याओं के दृष्टिकोण से विकसित श्रेणीबद्ध तंत्र की धारणा।
- 2. तर्क और आस्था का अनुपात.
स्कोलास्टिक दर्शन ने ईसाई शिक्षण के सार को न केवल विश्वास से, बल्कि तर्कसंगत आधार पर, और विज्ञान-दर्शन द्वारा भी समझने का कार्य निर्धारित किया है। तर्क और आस्था बहिष्कृत नहीं करते, बल्कि सत्य के ज्ञान के लिए मानव आत्मा की आकांक्षा में एक दूसरे की मदद करते हैं। और सत्य एक है - वह मसीह और उनकी शिक्षा है।
इस सत्य तक दो तरीकों से पहुंचा जा सकता है:
- - विश्वास से, रहस्योद्घाटन - एक छोटा, सीधा रास्ता;
- - तर्क के माध्यम से, विज्ञान - यह कई प्रमाणों के साथ एक लंबा रास्ता है।
- 3. सामान्य और एकल के बीच सहसंबंध की समस्याएं।
यह समस्या "ट्रिनिटी" की हठधर्मिता से जुड़ी है और इसे "नाममात्रवाद" के दृष्टिकोण से हल किया गया था (सामान्य केवल नाम में या मन में मौजूद है, एकल चीजें वास्तव में मौजूद हैं) या "यथार्थवाद" के दृष्टिकोण से ( सामान्य वास्तविकता में एक निश्चित सार के रूप में मौजूद होता है)।
थॉमस एक्विनास ने इस विवाद को अपने तरीके से हल किया:
- - सामान्य काफी यथार्थवादी रूप से मौजूद है, लेकिन मन में नहीं और प्लेटो के विचारों के रूप में नहीं;
- - ईश्वर में सामान्य। ईश्वर अस्तित्व की सामान्य परिपूर्णता है, अपने शुद्धतम रूप में सामान्य है;
- - सामान्य के क्षण किसी भी चीज़ में पाए जा सकते हैं, क्योंकि अस्तित्व में चीजें शामिल हैं;
- - कि एकल चीजें हैं, अर्थात्। अस्तित्व में है, उन्हें एक सामान्य समग्रता में बांधता है;
- - ईश्वर और अस्तित्व के माध्यम से व्यक्तिगत चीजों के संबंध (यानी, फिर से ईश्वर के माध्यम से) के अलावा कोई अन्य सामान्य चीज नहीं है।
- 1. मध्यकालीन दर्शन ईश्वरकेंद्रित है:
- - उनका विश्वदृष्टिकोण धार्मिक आस्था पर आधारित है;
- - दर्शन के केंद्र में - भगवान;
- 2. परन्तु दार्शनिक चिन्तन के क्षेत्र में यह कोई बंजर काल नहीं है। उनके विचारों ने पुनर्जागरण, नए युग और आधुनिक धार्मिक दर्शन की दार्शनिक प्रणालियों के विकास के आधार के रूप में कार्य किया:
- क) नाममात्रवादियों और यथार्थवादियों के बीच विवाद ने अनुभूति का एक नया विचार तैयार किया, इस प्रकार ज्ञानमीमांसा को अध्ययन के एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में उजागर किया गया;
- बी) अनुभवजन्य दुनिया के सभी विवरणों में नाममात्रवादियों की रुचि और अनुभव और प्रयोग के प्रति उनका रुझान बाद में पुनर्जागरण के भौतिकवादियों (एन. कॉपरनिकस, जे. ब्रूनो) और अनुभवजन्य दिशा के अंग्रेजी दार्शनिकों (एफ. बेकन) द्वारा जारी रखा गया। , टी. हॉब्स, जे. लोके).
- 3. यथार्थवाद के प्रतिनिधियों ने मानव मन की व्यक्तिपरक व्याख्या (17-18 शताब्दी के व्यक्तिपरक आदर्शवादी जे. बर्कले, डी. ह्यूम) की नींव रखी।
- 4. मध्यकालीन दर्शन ने आत्म-चेतना को एक विशेष व्यक्तिपरक वास्तविकता के रूप में "खोजा", जो बाहरी वास्तविकता की तुलना में किसी व्यक्ति के लिए अधिक विश्वसनीय और सुलभ है। "मैं" की दार्शनिक अवधारणा ने आकार लिया (यह नए युग के तर्कवाद के दर्शन में शुरुआती बिंदु बन गया - आर. डेसकार्टेस)।
- 5. मध्यकालीन नैतिकता ने मांस को उच्चतम आध्यात्मिक सिद्धांत के अधीन करने के लिए उसे शिक्षित करने का प्रयास किया (यह दिशा पुनर्जागरण के मानवतावाद द्वारा जारी रखी गई थी - एफ. पेट्रार्क, ई. रॉटरडैम)।
- 6. युगांतशास्त्रीय (दुनिया के अंत का सिद्धांत) दृष्टिकोण ने इतिहास के अर्थ को समझने की ओर ध्यान आकर्षित किया। हेर्मेनेयुटिक्स ऐतिहासिक ग्रंथों की व्याख्या करने की एक विशेष विधि के रूप में उभरा (मानवतावाद का राजनीतिक दर्शन पुनर्जागरण में आकार लिया)।
- 4. पुनर्जागरण और आधुनिक समय का दर्शन
पुनरुद्धार (पुनर्जागरण) - मध्य युग से नए समय (14 से 17 तक) में संक्रमण की अवधि।
युग की विशेषताएँ:
- 1. पूंजीवादी संबंधों का उदय, बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन।
- 2. राष्ट्र-राज्यों का निर्माण एवं पूर्ण राजतंत्रपश्चिमी यूरोप।
- 3. गहरे सामाजिक संघर्षों का युग (नीदरलैंड, इंग्लैंड में क्रांति का सुधार आंदोलन)।
- 4. खोज का युग (1492 - कोलंबस - अमेरिका; 1498 - वास्को डी गामा - अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, समुद्र के रास्ते भारत आया; 1519-1521 - फर्डिनेंड मैगलन - दुनिया भर में पहली यात्रा)।
- 5. संस्कृति और विज्ञान तेजी से धर्मनिरपेक्ष होते जा रहे हैं, यानी। धर्म के अविभाजित प्रभाव से मुक्त (लियोनार्डो दा विंची)।
- 1. पुनर्जागरण का दर्शन तीन कालखंडों से गुजरा:
I. काल - मानवतावादी (14वीं - 15वीं शताब्दी के मध्य)। (डांटे एलघिएरी, फ्रांसेस्को पेट्रार्का)।
द्वितीय. अवधि - नियोप्लेटोनिक (सेर। 15वीं - 16वीं शताब्दी)। (कुसा के निकोलस, पिको डेला मिरांडोला, पेरासेलसस)।
तृतीय. काल - प्राकृतिक दर्शन (16वीं - 17वीं शताब्दी का प्रारंभ)। (निकोलस कॉपरनिकस, जिओर्डानो ब्रूनो, गैलीलियो गैलीली)।
पुनर्जागरण के दर्शन की विशेषताएँ।
- 1. विद्वता-विरोधी चरित्र (हालाँकि राज्य के लिए विद्वतावाद आधिकारिक दर्शन बना रहा, और इसके सिद्धांतों का अध्ययन अधिकांश विश्वविद्यालयों में किया गया)। प्रस्तुत एक नई शैलीसोच रहा हूँ, जो अग्रणी भूमिकाविचार की अभिव्यक्ति के रूप (विद्वतवाद) को नहीं, बल्कि उसकी सामग्री को निर्दिष्ट करता है।
- 2. विश्वदृष्टि के मुख्य सिद्धांत के रूप में पंथवाद (नियोप्लाटोनिज्म के विचार का विकास - क्यूसा के निकोलस, मिरांडोलो, पेरासेलसस)। (पेंथिज़्म (ग्रीक पैन - सब कुछ और थियोस - भगवान) एक दार्शनिक सिद्धांत है जो "ईश्वर" और "प्रकृति" की अवधारणाओं को यथासंभव करीब लाता है)। ब्रह्मांड के पदानुक्रमित विचार को दुनिया की अवधारणा से बदल दिया गया है, जिसमें सांसारिक, प्राकृतिक और दैवीय सिद्धांतों का अंतर्संबंध होता है। प्रकृति आध्यात्मिक है.
- 3. मानवकेंद्रितवाद और मानवतावाद (डांटे एलघिएरी - "द डिवाइन कॉमेडी"; पेट्रार्क - "द बुक ऑफ सॉन्ग्स")।
नए दर्शन का सार मानवकेंद्रितवाद है। ईश्वर को नहीं, बल्कि मनुष्य को अब ब्रह्मांडीय अस्तित्व के केंद्र में रखा गया है। मनुष्य मात्र एक प्राकृतिक प्राणी नहीं है। वह समस्त प्रकृति का स्वामी, सृष्टिकर्ता है। शरीर की सुंदरता का पंथ इसे मानवकेंद्रितवाद से जोड़ता है।
दर्शन का कार्य मनुष्य में दैवीय और प्राकृतिक, आध्यात्मिक और भौतिक का विरोध नहीं है, बल्कि उनकी सामंजस्यपूर्ण एकता का प्रकटीकरण है।
मानवतावाद (लैटिन ह्यूमनिटास से - मानवता) पुनरुद्धार के लिए एक केंद्रीय सांस्कृतिक घटना है। मानवतावाद धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिवाद के प्रति स्वतंत्र सोच है। उन्होंने दर्शनशास्त्र की प्रकृति, सोच के स्रोत और शैली, एक वैज्ञानिक-सिद्धांतकार की छवि को बदल दिया (ये वैज्ञानिक, कवि, शिक्षक, राजनयिक हैं। जिन्होंने "दार्शनिक" नाम धारण किया)।
मानव रचनात्मक गतिविधि एक पवित्र (पवित्र) चरित्र प्राप्त करती है। वह एक निर्माता है, भगवान की तरह, वह एक नई दुनिया बनाता है और उसमें जो सर्वोच्च चीज़ है - वह स्वयं है।
- 4. पुनर्जागरण का प्राकृतिक दर्शन:
- * एन. कॉपरनिकस (1473-1543) - ब्रह्मांड का एक नया मॉडल बनाता है - हेलियोसेंट्रिज्म:
सूर्य की दुनिया का केंद्र;
संसार गोलाकार है, अथाह है, अनंत है;
सभी खगोलीय पिंड वृत्ताकार प्रक्षेपपथ में चलते हैं;
पृथ्वी, ग्रहों और तारों के साथ मिलकर एक एकल ब्रह्मांड बनाती है;
ग्रहों और पृथ्वी की गति के नियम समान हैं।
* जिओर्डानो ब्रूनो (1548-1600) - एन. कॉपरनिकस के सिद्धांत के दार्शनिक पहलू को विकसित करते हैं।
सूर्य ब्रह्माण्ड का केंद्र नहीं है, ऐसा कोई केंद्र है ही नहीं;
सूर्य केवल हमारे ग्रह मंडल का केंद्र है;
ब्रह्माण्ड की कोई सीमा नहीं है, इसमें विश्वों की संख्या अनंत है;
अन्य ग्रहों पर जीवन और बुद्धि है;
ब्रह्माण्ड ईश्वर के समान है, ईश्वर भौतिक जगत में ही घिरा हुआ है।
- (17 फरवरी 1600 को फूलों के मैदान पर जला दिया गया)।
- * गैलीलियो गैलीली (1564-1642) - ब्रह्मांड का अध्ययन जारी रखा, दूरबीन का आविष्कार किया, गणित का उपयोग करके वैज्ञानिक विश्लेषण की एक विधि विकसित की, इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञान का संस्थापक माना जाता है।
- (इनक्विजिशन के कैदी बने रहकर ही उनकी मृत्यु हो गई)।
- 5. पुनर्जागरण का सामाजिक दर्शन।
पुनर्जागरण दर्शन ने मौलिक ग्रंथ प्रस्तुत किये ऐतिहासिक प्रक्रियाऔर सामाजिक समानता के विचार से जुड़े एक आदर्श राज्य की परियोजनाएँ।
* निकोलो डि बर्नार्डो मैकियावेली (1469-1527) - फ्लोरेंस गणराज्य के एक उच्च अधिकारी, राजनयिक, सैन्य सिद्धांतकार थे। कार्यवाही: "टाइटस लिवियस के पहले दशक पर प्रवचन" और "सॉवरेन"।
सार्वजनिक जीवन में दैवीय पूर्वनियति के विचार को पूरी तरह से खारिज करता है;
राजनीतिक प्रणालियाँ जन्म लेती हैं, महानता और शक्ति प्राप्त करती हैं, और फिर क्षय, क्षय और नष्ट हो जाती हैं, अर्थात। वे एक शाश्वत चक्र में हैं, ऊपर से किसी पूर्व-स्थापित लक्ष्य के अधीन नहीं हैं। समाज, राज्य और नैतिकता के उद्भव को घटनाओं के प्राकृतिक पाठ्यक्रम द्वारा समझाया गया है।
* थॉमस मोरे (1478-1535) - यूटोपियन समाजवाद के संस्थापक। इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर. श्रम: "यूटोपिया" (यूटोपिया के शानदार द्वीप की आदर्श संरचना का विवरण (ग्रीक से; शाब्दिक रूप से "कहीं नहीं" - एक जगह जो अस्तित्व में नहीं है - टी. मोर द्वारा गढ़ा गया एक शब्द))।
सभी प्रकार की निजी संपत्ति का विनाश;
सभी नागरिकों का अनिवार्य श्रम;
राज्य निकायों का चुनाव;
परिवार साम्यवादी जीवन की कोशिका है।
* टोमासो कैम्पानेला (1568-1639) - डोमिनिकन भिक्षु, स्पेनियों के शासन से इटली की मुक्ति के संघर्ष में भागीदार। 27 साल जेल में. श्रम: "सूर्य का शहर" - एक साम्यवादी स्वप्नलोक।
निजी संपत्ति और परिवार का उन्मूलन;
बच्चों का पालन-पोषण राज्य द्वारा किया जाता है;
अनिवार्य 4 घंटे का श्रम;
आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों का वितरण;
विज्ञान, शिक्षा, श्रम शिक्षा का विकास;
ज्ञान की दृष्टि से उत्कृष्ट व्यक्ति को राज्य का मुखिया चुना जाता है;
विश्वव्यापी एकता, राज्यों और लोगों का एक संघ बनाने की आवश्यकता, जो लोगों के बीच भ्रातृहत्या युद्धों की समाप्ति सुनिश्चित करे।
- 1) पुनर्जागरण के दर्शन का सार मानवकेंद्रितवाद है। मनुष्य को निर्माता माना जाता है।
- 2) हालाँकि पुनर्जागरण ने महान दार्शनिकों को नहीं छोड़ा, और दार्शनिक रचनात्मकता मुख्य रूप से "आधुनिकीकरण स्मरण" के रूप में सामने आई, यह:
प्राकृतिक मानव मन में विश्वास के विचार की पुष्टि की;
धर्म से मुक्त दर्शन की नींव रखी।
परंपरागत रूप से, नये युग के दर्शन को तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है:
- प्रथम काल: 17वीं शताब्दी का अनुभववाद और तर्कवाद।
- दूसरा कालखंड: 18वीं सदी का ज्ञानोदय दर्शन।
- तीसरी अवधि: जर्मन शास्त्रीय दर्शन।
प्रत्येक काल की अपनी विशेषताएं होती हैं, जो उस ऐतिहासिक चरण में समाज की स्थिति से निर्धारित होती हैं।
ए) 17वीं शताब्दी का अनुभववाद और तर्कवाद:
ऐतिहासिक स्थितियाँ:
- 1) सामंती समाज का बुर्जुआ समाज द्वारा प्रतिस्थापन (नीदरलैंड, इंग्लैंड में क्रांति)।
- 2) चर्च की आध्यात्मिक तानाशाही का कमजोर होना (प्रोटेस्टेंटवाद का विकास)।
- 3) भौतिक उत्पादन के अभ्यास के साथ विज्ञान का संबंध।
- - टोरिसेली - पारा बैरोमीटर, वायु पंप;
- - न्यूटन - यांत्रिकी के बुनियादी नियम तैयार किए;
- - बॉयल - रसायन विज्ञान में प्रयुक्त यांत्रिकी।
ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण जन चेतना में परिवर्तन आया:
- 1. पश्चिमी यूरोपदो रास्तों से ऐतिहासिक विकाससभ्यता (आध्यात्मिक या वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति) वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का मार्ग चुनती है।
- 2. विज्ञान और दर्शन के कार्यों की एक नई समझ विकसित हुई है - "विज्ञान के लिए विज्ञान" नहीं, बल्कि प्रकृति पर मनुष्य की शक्ति बढ़ाने के लिए विज्ञान।
- 3. अनुभूति के नए तरीकों की खोज सक्रिय कर दी गई है:
- - बड़ी संख्या में तथ्यों का व्यवस्थितकरण;
- - दुनिया की एक समग्र तस्वीर बनाना;
- - प्राकृतिक घटनाओं के बीच कारण संबंधों की स्थापना।
इसलिए, इस काल के दर्शन में मुख्य समस्याएँ ज्ञान के सिद्धांत (एपिस्टेमोलॉजी) की समस्याएँ हैं:
- - जानने का क्या मतलब है?
- - जो सत्य का मार्ग प्रशस्त करता है:
- -संवेदना या मन;
- - अंतर्ज्ञान या तर्क.
- - अनुभूति विश्लेषणात्मक या सिंथेटिक होनी चाहिए।
"शुद्ध कारण" का विचार उत्पन्न होता है, अर्थात्। "मूर्तियों" से मुक्त एक मन जो घटना के सार में प्रवेश करता है।
दार्शनिक सक्रिय रूप से सत्य की खोज कर रहे हैं, मुख्य विधिज्ञान, जो शाश्वत सत्य की ओर ले जाएगा, पूर्ण, निरपेक्ष, सभी लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त।
नई पद्धति का आधार खोजा जा रहा है:
- 1) संवेदी अनुभव में, अनुभवजन्य आगमनात्मक ज्ञान (बेकन, हॉब्स, लॉक) के महत्व से परे विचार को आगे बढ़ाना।
- 2) बुद्धि में, जो तार्किक निगमनात्मक-गणितीय ज्ञान देता है जो मानव अनुभव के लिए कम नहीं है (डेसकार्टेस, स्पिनोज़ा, लाइबनिज़)।
सबसे महत्वपूर्ण अनुभववादियों की दार्शनिक प्रणालियाँ थीं: एफ. बेकन, टी. हॉब्स, तर्कवादी: आर. डेसकार्टेस, बी. स्पिनोज़ा, जी. लीबनिज़।
- 1. अनुभववादियों (फ्रांसिस बेकन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक) का मानना था कि: * ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है
- - अनुभव हमारी कामुकता, संवेदनाओं, धारणाओं, विचारों से जुड़ा है;
- - मनुष्य और मानव जाति के सभी ज्ञान की सामग्री अंततः अनुभव में आती है।
- - किसी व्यक्ति की आत्मा और दिमाग में कोई जन्मजात ज्ञान, विचार या विचार नहीं होते हैं।
- - किसी व्यक्ति की आत्मा और दिमाग शुरू में मोम की गोली की तरह शुद्ध होते हैं, और पहले से ही संवेदनाएं और धारणाएं इस गोली पर अपने "अक्षर" लिखती हैं।
- - चूंकि संवेदनाएं हमें धोखा दे सकती हैं, इसलिए हम उन्हें एक प्रयोग के माध्यम से जांचते हैं जो इंद्रियों के डेटा को सही करता है।
- - ज्ञान को शुद्ध, प्रायोगिक (प्रायोगिक) से सामान्यीकरण और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की ओर जाना चाहिए, यह प्रयोग के साथ-साथ मन को आगे बढ़ाने की प्रेरक विधि है - और दर्शन और सभी विज्ञानों में सच्ची विधि है।
- ए) फ्रांसिस बेकन (1561-1626) - इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर, विस्काउंट।
कार्य: "न्यू ऑर्गन" - विज्ञान के विकास की समस्याएं और वैज्ञानिक ज्ञान का विश्लेषण।
- 1. दर्शनशास्त्र एवं समस्त विज्ञान का व्यावहारिक महत्व। "ज्ञान ही शक्ति है" उनका कथन है।
- 2. अनुभूति की मुख्य विधि अनुभव और प्रयोग पर आधारित प्रेरण है। "हमारा विचार एकल तथ्यों के ज्ञान से वस्तुओं और प्रक्रियाओं के पूरे वर्ग के ज्ञान की ओर बढ़ता है।"
- 3. सभी ज्ञान का आधार अनुभव (अनुभव) है, जिसे तदनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए और एक विशिष्ट लक्ष्य के अधीन होना चाहिए।
- 4. विज्ञान जिन तथ्यों पर निर्भर करता है उन्हें उसकी विधि (इंडक्शन) का उपयोग करके वर्गीकृत किया जा सकता है। उनका मानना था कि लोगों की तुलना इनसे नहीं की जानी चाहिए:
- - मकड़ियाँ जो स्वयं से एक धागा बुनती हैं (अर्थात "शुद्ध चेतना" से सत्य को इस प्रकार निकालती हैं);
- - चींटियाँ जो केवल संग्रह करती हैं (अर्थात तथ्यों के संग्रह की प्रतीक्षा करती हैं);
उन्हें मधुमक्खियों की तरह होना चाहिए जो एकत्र होती हैं और संगठित होती हैं (अर्थात यह अनुभववाद से सिद्धांत की ओर उत्थान है)।
- 5. तर्कवाद की आलोचना करते हुए, उन्होंने मानव जाति को चार "मूर्तियों" के खिलाफ चेतावनी दी, अर्थात्। मन की बुरी आदतें जो त्रुटियों को जन्म देती हैं:
- - "परिवार की मूर्तियाँ" - अर्थात। मानव जाति में निहित अभिविन्यास (विशेष रूप से, चीजों में मौजूद व्यवस्था से अधिक बड़े क्रम की अपेक्षा);
- - "गुफा की मूर्तियाँ" - एक व्यक्तिगत शोधकर्ता में निहित व्यक्तिगत अंधविश्वास;
- - "बाज़ार की मूर्तियाँ" - भाषा में बुरे शब्दों का प्रयोग जो हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं;
- - "थिएटर की मूर्तियाँ" - वे जो आम तौर पर स्वीकृत विचार प्रणालियों (वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक) से जुड़ी हैं।
- बी) अंग्रेजी दार्शनिक टी. हॉब्स (1588-1679) के व्यक्तित्व में, बेकन के भौतिकवाद को अपना रक्षक और उत्तराधिकारी मिला। हॉब्स के अनुसार पदार्थ शाश्वत है और अलग-अलग शरीर अस्थायी हैं। उन्होंने पदार्थ की गति को अंतरिक्ष में पिंडों की गति के समान माना, अर्थात्। एक यांत्रिक गति के रूप में, और इस तंत्र की तुलना न केवल प्रकृति के सभी निकायों से की जाती है, बल्कि मनुष्य और समाज से भी की जाती है।
बेकन के विपरीत, हॉब्स ने धर्म को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया और इसे विज्ञान के साथ असंगत माना। सार्वजनिक जीवन में धर्म का स्थान "जनता पर अंकुश लगाने" के साधन के रूप में है।
- सी) अंग्रेजी दार्शनिक जे. लॉक (1632-1704) ने हमारे ज्ञान के स्रोत के रूप में संवेदनाओं के सिद्धांत को विकसित किया। लोग साथ पैदा नहीं होते तैयार विचार. नवजात शिशु का सिर एक खाली बोर्ड है जिस पर जीवन अपने पैटर्न - ज्ञान खींचता है। मन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले इन्द्रियों में न हो, ऐसी लॉक की मुख्य थीसिस है। जन्मजात और सामाजिक की द्वंद्वात्मकता को रेखांकित करते हुए, लॉक ने बड़े पैमाने पर शिक्षाशास्त्र और मनोविज्ञान के विकास को निर्धारित किया।
- 2. तर्कवादी - रेने डेसकार्टेस, बेनेडिक्ट स्पिनोज़ा, गॉटफ्राइड लीबनिज का मानना था कि:
- - मानवीय संवेदनाओं पर आधारित अनुभव सामान्य वैज्ञानिक पद्धति का आधार नहीं हो सकता।
A. धारणाएँ और संवेदनाएँ भ्रामक हैं;
बी. प्रायोगिक डेटा, प्रयोगात्मक डेटा की तरह, हमेशा संदिग्ध होते हैं।
- - लेकिन हमारे मन में, हमारी आत्मा में सहज रूप से स्पष्ट और विशिष्ट विचार हैं।
- - मुख्य बात यह है कि एक व्यक्ति सोचता है। यह मुख्य है - सहज (अनुभवहीन) विचार यह है: "मुझे लगता है - इसलिए, मेरा अस्तित्व है" (आर. डेसकार्टेस)।
- - फिर, कटौती के नियमों के अनुसार (सामान्य से विशेष तक), हम ईश्वर, प्रकृति, अन्य लोगों के अस्तित्व की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं।
- - निष्कर्ष क्या है:
- ए) मानव मस्तिष्क में कई विचार होते हैं (किसी भी अनुभव की परवाह किए बिना, यानी ये विचार संवेदनाओं से पहले संवेदनाओं के बिना उत्पन्न हुए)।
- बी) मन में निहित विचारों को विकसित करके, हम दुनिया के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं (हालांकि एक व्यक्ति संवेदनाओं से दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, इसलिए अनुभव और प्रयोग दुनिया के बारे में ज्ञान के महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन सत्य का आधार हैं) विधि मन में ही खोजी जानी चाहिए)।
- ग) सोच प्रेरण और कटौती पर आधारित है। यह स्वतंत्र रूप से और संवेदना से पहले उत्पन्न होता है, लेकिन सोच संवेदनाओं पर लागू होती है।
- घ) सभी विज्ञानों और दर्शन की सच्ची विधि कुछ हद तक गणितीय विधियों के समान है।
- - वे प्रत्यक्ष अनुभव के बाहर दिए जाते हैं, वे सामान्य, अत्यंत स्पष्ट और सटीक फॉर्मूलेशन से शुरू होते हैं, जहां वे सामान्य विचारों से विशेष निष्कर्षों तक जाते हैं और गणित में कोई प्रयोग नहीं होता है।
- ए) रेने डेसकार्टेस (1596-1650) - फ्रांसीसी दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ।
"प्रथम दर्शन पर चिंतन", "दर्शन के सिद्धांत", "मन की दिशा के लिए नियम", "विधि पर प्रवचन", "आध्यात्मिक चिंतन"।
- 1) अस्तित्व के सिद्धांत में, संपूर्ण निर्मित विश्व को दो प्रकार के पदार्थों में विभाजित किया गया है: आध्यात्मिक और भौतिक।
- - आध्यात्मिक - अविभाज्य पदार्थ
- - पदार्थ - अनंत से विभाज्य
दोनों पदार्थ एक-दूसरे के बराबर और स्वतंत्र हैं (जिसके परिणामस्वरूप डेसकार्टेस को द्वैतवाद का संस्थापक माना जाता है)।
- 2) विकसित ज्ञानमीमांसा:
- - अनुभूति की प्रक्रिया की शुरुआत - संदेह
- - एक निगमनात्मक विधि विकसित की।
- बी) डच दार्शनिक बी. स्पिनोज़ा (1632-1677) की शिक्षा मौलिक थी। उन्होंने उस समय के विचारों को श्रद्धांजलि देते हुए माना कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन वह किसी भी व्यक्तित्व लक्षण से रहित है। ईश्वर प्रकृति है, विस्तार और सोच रखता है। सारी प्रकृति सोच सकती है, मानव सोच सामान्य रूप से सोचने का एक विशेष मामला है।
स्पिनोज़ा ने आवश्यकता और स्वतंत्रता की समस्या पर भी बहुत ध्यान दिया।
यह उन्हीं का शब्द है: "स्वतंत्रता एक सचेत आवश्यकता है।"
- ग) जर्मन दार्शनिक जी. लीबनिज (1646-1716) ने प्लेटोनिक विरासत में अंतर्निहित वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के विचारों को विकसित किया। लीबनिज का मानना था कि दुनिया सबसे छोटे तत्वों - भिक्षुओं से बनी है। सन्यासी अस्तित्व के आध्यात्मिक तत्व हैं, उनमें गतिविधि और स्वतंत्रता है, वे निरंतर परिवर्तन में हैं और पीड़ा, धारणा और चेतना में सक्षम हैं। ईश्वर भिक्षुओं की एकता और सुसंगति को नियंत्रित करता है। इस प्रकार, निचले भिक्षुओं में केवल अस्पष्ट विचार निहित हैं (अकार्बनिक और पौधे की दुनिया ऐसी स्थिति में है); जानवरों में, प्रतिनिधित्व संवेदना के चरण तक पहुँचते हैं, और मनुष्य में - एक स्पष्ट समझ, कारण।
- 3. व्यक्तिपरक आदर्शवाद का विकास अंग्रेजी दार्शनिक जे. बर्कले और डी. ह्यूम के कार्यों में हुआ था।
- ए) धर्म के कट्टर समर्थक जे. बर्कले (1685-1753) ने पदार्थ की अवधारणा की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि पदार्थ की अवधारणा सामान्य है और इसलिए गलत है। बर्कले ने तर्क दिया, हम पदार्थ को इस रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि केवल चीजों के व्यक्तिगत गुणों - स्वाद, गंध, रंग, आदि को देखते हैं, जिसकी धारणा को बर्कले ने "विचार" कहा है। हमारे आस-पास की चीज़ें ईश्वर के मन में विचारों के रूप में मौजूद हैं, जो सांसारिक जीवन का कारण और स्रोत हैं।
- बी) डी. ह्यूम (1711-1776) ने भी व्यक्तिपरक-आदर्शवादी विकसित किया, लेकिन बर्कले से कुछ अलग।
यह पूछे जाने पर कि क्या बाहरी दुनिया का अस्तित्व है, ह्यूम ने स्पष्ट उत्तर दिया: "मुझे नहीं पता।" वह इस तथ्य से आगे बढ़े कि एक व्यक्ति बाहरी दुनिया के बारे में डेटा केवल संवेदनाओं से प्राप्त करता है, और संवेदनाएं लगातार बदल रही हैं। इसलिए निष्कर्ष: वस्तुनिष्ठ ज्ञान असंभव है। यहीं से ज्ञानवाद जैसी दार्शनिक दिशा की उत्पत्ति होती है।
- 1. इस काल के दार्शनिकों ने वैज्ञानिक ज्ञान के तरीकों को विकसित करके प्रकृति के अध्ययन में विज्ञान की ज्ञानमीमांसीय संभावनाओं को मजबूत किया, जिससे व्यक्ति को अपनी शक्तियों के उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ।
- 2. प्रभाव में होना प्राकृतिक विज्ञान 17वीं शताब्दी में विश्वदृष्टिकोण बदल गया। इसे दुनिया को तार्किक रूप से जुड़े और गणितीय रूप से सटीक रूप से वर्णित घटक तत्वों में विभाजित करने की अनुमति दी गई थी।
- 3. तर्कवाद और अनुभववाद के बीच प्रतिद्वंद्विता के दौरान, तर्कवाद प्रबल हुआ, जिसकी बदौलत सोच के सिद्धांत के स्पष्ट तंत्र की नींव रखी गई, भविष्य के गणितीय और द्वंद्वात्मक तर्क के लिए पूर्वापेक्षाएँ बनाई गईं।
- 4. आगे विकास सामाजिक आशावाद की समस्याओं, प्राकृतिक मानवाधिकारों के बारे में विचारों, सामाजिक अनुबंध, रूपों से हुआ राज्य संरचना, उसके चारों ओर की दुनिया में मनुष्य का स्थान।
बी. आत्मज्ञान का दर्शन 18...
- 6. सामाजिक संबंधों और सार्वजनिक चेतना में परिवर्तन ने मन की मुक्ति, सामंती-धार्मिक विचारधारा से मुक्ति, एक नए विश्वदृष्टि के गठन के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में कार्य किया।
- 7. सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष जो 18वीं शताब्दी में महान फ्रांसीसी बुर्जुआ क्रांति (1789-1794) की पूर्व संध्या पर सामने आया।
इसे ध्यान में रखते हुए, 18वीं शताब्दी में दार्शनिक अनुसंधान का केंद्र इंग्लैंड से फ्रांस (और फिर जर्मनी) में स्थानांतरित हो गया।
फ्रांस में:
- - ज्वलंत मुद्दों के लिए दार्शनिकों के सक्रिय कार्य, पुराने सामंती और लिपिक विचारों के स्पष्ट और त्वरित खंडन की आवश्यकता थी;
- - दर्शन विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के कार्यालयों की दीवारों से परे चला गया, यह पेरिस के धर्मनिरपेक्ष सैलून में, दर्जनों और सैकड़ों प्रतिबंधित प्रकाशनों के पन्नों तक चला गया;
- - दर्शनशास्त्र विचारकों और राजनेताओं के लिए एक विषय बन जाता है;
- - उचित आधार पर विज्ञान के पुनर्गठन का विचार विकसित हो रहा है:
- - शिक्षित लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच प्रकृति और समाज के बारे में सकारात्मक, व्यावहारिक रूप से उपयोगी ज्ञान का प्रसार;
- - शासकों (सम्राटों) को विज्ञान और दर्शन की नवीनतम उपलब्धियों से परिचित कराना, जो राज्यों में कारण के सिद्धांत का परिचय देगा;
- - पारंपरिक ईसाई धर्म की आलोचना और धार्मिक हठधर्मिता के खिलाफ लड़ाई।
ज्ञानोदय के दर्शन की विशेषताएँ:
- 1. बुद्धिवाद. बुद्धिवाद की व्याख्या एक ज्ञानमीमांसीय सिद्धांत के रूप में की जाती है, जिसमें कहा गया है कि अनुभूति का मुख्य उपकरण मन है, अनुभूति में संवेदनाएं और अनुभव द्वितीयक महत्व के हैं।
- 2. सभी दार्शनिक स्कूलों और प्रणालियों के केंद्र में, एक नियम के रूप में, एक सक्रिय विषय है, जो अपने दिमाग के अनुसार दुनिया को पहचानने और बदलने में सक्षम है।
- - बुद्धिवादी प्रणालियों में मन को व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तिपरक गतिविधि माना जाता है।
- - एक तर्कसंगत प्राणी के रूप में, तर्कवाद के दृष्टिकोण से, एक व्यक्ति को दुनिया का शासक बनने, उचित आधार पर सामाजिक संबंधों का पुनर्निर्माण करने के लिए कहा जाता है।
- - संसार वैध है, स्व-व्यवस्थित है, स्व-प्रजनन है - यह पदार्थ की आंतरिक गतिविधि, उसकी सामान्य गति से जुड़ा है।
- - फ्रांसीसी भौतिकवाद की यंत्रवत प्रकृति। ठोस पिंडों की यांत्रिकी के नियमों, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को सार्वभौमिक स्तर तक ऊपर उठाया गया और उन्होंने सभी प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं को निर्धारित किया। (जे. लैमेट्री "मैन-मशीन")।
फ्रांसीसी प्रबुद्धता के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि:
- * फ्रेंकोइस वोल्टेयर (1694-1778)
- * जीन जैक्स रूसो (1712-1778)
- * डेनिस डिडेरॉट (1713-1784) (35 खंड विश्वकोश के निर्माता)
- * जूलियन ला मेट्री (1709-1751)
- * क्लाउड गैल्वेटियस (1715-1771)
- * पॉल होल्बैक (1723-1789)
बी. जर्मन शास्त्रीय दर्शन (18वीं सदी के अंत - 19वीं सदी के मध्य)।
ऐतिहासिक स्थितियाँ.
- 1. यूरोप और अमेरिका में शांति तेजी से और लगातार एक औद्योगिक सभ्यता का रूप ले रही है। उद्योग में प्रगति प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करती है:
- 1784 - वाट का सार्वभौमिक भाप इंजन प्रकट हुआ;
- 1800 - ए. वोल्टा ने एक रासायनिक धारा स्रोत का आविष्कार किया;
- 1807 - पहली स्टीमबोट;
- 1825 - पहला भाप इंजन;
- 1832 - एल. शिलिंग - विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ;
- 1834 - एम. जी. जैकोबी - विद्युत मोटर, आदि।
- 2. प्राकृतिक विज्ञान में, यांत्रिकी अपनी पूर्व प्रमुख भूमिका खो रही है:
- - 18वीं शताब्दी के अंत तक, रसायन विज्ञान का गठन प्राकृतिक पदार्थों के गुणात्मक परिवर्तनों के विज्ञान के रूप में किया गया था;
- - जीव विज्ञान और विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत बन रहा है।
- 3. विकसित यूरोपीय देशों में हो रहे तूफानी सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों का जर्मनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा:
- - जर्मनी, उस काल के फ्रांस और इंग्लैंड के विपरीत, एक आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा देश बना रहा, जो 360 स्वतंत्र राज्यों ("जर्मन राष्ट्र का पवित्र रोमन साम्राज्य") में विभाजित था;
- - उसने गिल्ड प्रणाली, दासता के अवशेष रखे;
- - चांसलर बिस्मार्क के कठोर राजनीतिक आदेश ने व्यक्तिगत आत्म-अभिव्यक्ति, रचनात्मकता की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता के लिए एकमात्र क्षेत्र छोड़ दिया: कारण का क्षेत्र।
विज्ञान की प्रगति, यूरोप में क्रांतियों का अनुभव (विशेषकर) फ्रेंच क्रांति 1789-1794) ने दार्शनिक और सैद्धांतिक सोच के विकास के लिए आवश्यक शर्तें तैयार कीं, जिसके परिणामस्वरूप आदर्शवादी द्वंद्वात्मकता का विकास (शास्त्रीय जर्मन दर्शन के ढांचे के भीतर) हुआ।
जर्मन शास्त्रीय दर्शन की विशेषताएं:
- 1. मुख्य दार्शनिक पदों की विविधता के बावजूद, जर्मन शास्त्रीय दर्शन दर्शन के विकास में एक एकल, अपेक्षाकृत स्वतंत्र चरण है, क्योंकि इसकी सभी प्रणालियाँ एक दूसरे से अनुसरण करती हैं, अर्थात। एक निश्चित निरंतरता के संरक्षण के साथ, पिछले एक को नकार दिया गया।
- 2. द्वंद्वात्मक परंपराओं का पुनरुद्धार (प्राचीन विरासत की अपील के माध्यम से)। यदि कांट की द्वन्द्वात्मकता अधिक है नकारात्मक मूल्यशुद्ध कारण का "परिष्कार", फिर बाद के दार्शनिकों और विशेष रूप से हेगेल में, यह तार्किक श्रेणियों की एक अभिन्न प्रणाली तक बढ़ जाता है।
- 3. वस्तुनिष्ठ और पारलौकिक आदर्शवाद (कांट) से द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद में संक्रमण (फिचटे और शेलिंग से हेगेल तक)।
- 4. पारंपरिक "तर्कसंगत" तत्वमीमांसा की आलोचना और दर्शन को वैज्ञानिक ज्ञान की एक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा ("विज्ञान" फिचटे, "दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश" हेगेल)।
- 5. इतिहास को एक दार्शनिक समस्या के रूप में देखना और इतिहास के अध्ययन के लिए हेगेल द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति का अनुप्रयोग।
जर्मन शास्त्रीय दर्शन का प्रतिनिधित्व प्रमुख दार्शनिकों द्वारा किया जाता है:
- * कांट
- * फिचटे
- * स्केलिंग
- *हेगेल
- * फ्यूअरबैक
- ए) इमैनुएल कांट (1724-1804) - जर्मन शास्त्रीय दर्शन के संस्थापक - कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय के रेक्टर, एक व्यक्तिपरक आदर्शवादी।
उनके दार्शनिक शिक्षण में, दो चरण स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं: पूर्व-महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक।
सबक्रिटिकल स्टेज (सहज-भौतिकवादी):
उन्होंने भंवर घूर्णी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप, फैली हुई गैस और धूल पदार्थ से सौर मंडल के प्राकृतिक गठन का एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत विकसित किया है।
गंभीर अवस्था (1770 से)।
कृतियाँ: शुद्ध कारण की आलोचना, व्यावहारिक कारण की आलोचना, निर्णय की आलोचना।
- 1. केंद्रीय समस्या मानव अनुभूति की संभावनाओं और उसकी सीमाओं की स्थापना की समस्या है
- - अनुभूति की प्रक्रिया, संज्ञान लेने वाले विषय की सोच में संज्ञेय वस्तुओं के एक प्रकार के निर्माण की एक सक्रिय रचनात्मक प्रक्रिया है, जो अपने स्वयं के कानूनों के अनुसार आगे बढ़ती है।
- - दर्शनशास्त्र में पहली बार, संज्ञेय पदार्थ की संरचना पर विचार नहीं किया गया, बल्कि संज्ञेय विषय की विशिष्टता पर विचार किया गया - अनुभूति की विधि और विषय दोनों को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक के रूप में।
"कोपरनिकन तख्तापलट", अर्थात्। कांट के अनुसार, "यह मन नहीं था, जो सूर्य की तरह दिखावे की दुनिया के चारों ओर घूमता था, बल्कि दिखावे की दुनिया मन के चारों ओर घूमती थी।"
- - आवश्यक शर्तेंज्ञान मानव मस्तिष्क में प्राथमिकता (अर्थात अनुभव से पहले) रखा जाता है और ज्ञान का आधार बनता है।
- - लेकिन मानव मस्तिष्क ज्ञान की सीमाएँ भी निर्धारित करता है। कांट ने मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले के बीच अंतर किया:
- - चीजों की घटना;
- - चीज़ें अपने आप।
हम दुनिया को वैसा अनुभव नहीं करते जैसा वह है, बल्कि वैसा अनुभव करते हैं जैसा हम उसे देखते हैं। हम चीजों की परिघटना (घटना) देखते हैं, लेकिन किसी चीज के बारे में पूर्ण ज्ञान असंभव है, वह अपने आप में एक चीज बनी रहती है (संज्ञा), इससे दुनिया को जानने की असंभवता के बारे में निष्कर्ष निकलता है, यानी। अज्ञेयवाद
- 2. मानी गई योजना व्यावहारिक अनुप्रयोगकारण या नैतिकता
- - इसका प्रारंभिक आधार यह दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक साध्य है (यह समस्याओं को हल करने का एक साधन नहीं है, यहां तक कि आम अच्छे के नाम पर भी)।
- - कांट की नैतिकता का मुख्य नियम एक स्पष्ट अनिवार्यता है: किसी कार्य को केवल तभी नैतिक माना जा सकता है जब वह दूसरों के लिए कानून बन सकता है।
काम
- - यदि यह खुशी, प्रेम, सहानुभूति आदि की इच्छा पर आधारित है तो नैतिक नहीं है;
- - नैतिक है यदि यह कर्तव्य के पालन और नैतिक कानून के प्रति सम्मान पर आधारित है।
भावनाओं और नैतिक कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में, कांट नैतिक कर्तव्य के प्रति बिना शर्त आज्ञाकारिता की मांग करता है।
बी) जोहान गोटलिब फिच्टे (1762-1814) - बर्लिन विश्वविद्यालय के पहले रेक्टर। व्यक्तिपरक आदर्शवादी.
- 1. फिचटे ने विषय के प्रति व्यावहारिक-सक्रिय दृष्टिकोण से प्राप्त किसी भी सिद्धांत, किसी भी चिंतन को गौण माना।
- 2. चेतना स्वयं उत्पन्न होती है। यह कभी पूरा नहीं होता, यह हमेशा एक प्रक्रिया बनकर रह जाती है।
- 3. चेतना न केवल स्वयं का, बल्कि पूरे विश्व का निर्माण करती है - कल्पना की अंधी, अचेतन शक्ति से
- 4. दुनिया के साथ चेतना के सक्रिय, सक्रिय संबंध से, उन्होंने विरोधों की एकता ("मैं" और "नहीं - मैं" का अनुपात) और द्वंद्वात्मकता की अन्य श्रेणियों का सिद्धांत प्राप्त किया।
- 5. उसके लिए "मैं" और "नहीं - मैं" ही संसार है।
- - "मैं" आत्मा, इच्छा, नैतिकता है
- - "नहीं-मैं" प्रकृति और पदार्थ है।
- 6. मनुष्य की मुख्य समस्या नैतिकता है।
- 7. जीवन का मुख्य रूप सामाजिक सांस्कृतिक कार्य है।
- सी) शेलिंग फ्रेडरिक विल्हेम जोसेफ (1775-1854) - बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एक वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी।
- 1. उन्होंने द्वंद्वात्मकता की अवधारणा को न केवल चेतना तक, बल्कि प्रकृति तक भी विस्तारित किया:
- - प्रकृति किसी व्यक्ति के नैतिक लक्ष्यों को साकार करने का साधन नहीं है, मानव गतिविधि के लिए "सामग्री" नहीं है।
- - प्रकृति मन के अचेतन जीवन का एक रूप है, जो मूल रूप से एक शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति से संपन्न है जो चेतना उत्पन्न करती है। प्रकृति एक "पथरी हुई बुद्धि" है।
- 2. अनुभूति और, सामान्य तौर पर, सभी मानव गतिविधियों को स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा यदि प्रकृति को आत्मा, कारण के साथ समान नहीं माना जाता है। निरपेक्ष आदर्श और यथार्थ की पहचान है। इसलिए, केवल एक दार्शनिक या प्रतिभा प्रेरणा के परमानंद में एक कवि (तर्कहीन रूप से) निरपेक्ष को पहचान सकता है।
- डी) जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक (1770-1831) - बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर - जर्मन आदर्शवाद के शिखर।
कार्यवाही: "आत्मा की घटना विज्ञान", "दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश", "कानून का दर्शन", "दर्शनशास्त्र के इतिहास पर व्याख्यान", "इतिहास के दर्शन पर व्याख्यान", आदि।
- 1. "फेनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट" में उन्होंने मानव चेतना के विकास को उसकी पहली झलक से लेकर विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति (घटना विज्ञान - उनके ऐतिहासिक विकास में चेतना की घटना (घटना) का सिद्धांत) की जागरूक महारत तक माना।
- 2. परस्पर जुड़े विचारों के रूप में एक दर्शन का निर्माण किया। हेगेल के विचार अवधारणाओं सहित किसी भी चीज़ का तरीका हैं। यह वस्तु और विषय दोनों का सार है, इसलिए विचार में विषय और विषय का विरोध दूर हो जाता है। संपूर्ण विश्व का विकास निरपेक्ष विचार का विकास है, जो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का आधार है:
- - विचार प्राथमिक है;
- - वह सक्रिय और सक्रिय है;
- - इसकी गतिविधि आत्म-ज्ञान में निहित है।
पूर्ण विचार अपने आत्म-ज्ञान में तीन चरणों से गुजरता है:
- 1) किसी विचार का विकास उसके अपने हृदय में, "शुद्ध सोच के तत्व" में - तर्क, जहां विचार अपनी सामग्री को एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे से गुजरने वाली तार्किक श्रेणियों की प्रणाली में प्रकट करता है;
- 2) "अन्यता" के रूप में विचार का विकास, अर्थात्। प्रकृति के स्वरूप में, प्रकृति का दर्शन; प्रकृति विकसित नहीं होती है, बल्कि केवल तार्किक श्रेणियों के आत्म-विकास की बाहरी अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करती है जो इसके आध्यात्मिक सार को बनाती है;
- 3) विचार और इतिहास में विचार का विकास - निरपेक्ष आत्मा का रूप लेना - आत्मा का दर्शन। इस स्तर पर, निरपेक्ष विचार फिर से अपने पास लौट आता है और तीन चरणों से गुजरते हुए विभिन्न प्रकार की मानव चेतना और गतिविधि में अपनी सामग्री को समझता है:
- प्रथम - व्यक्तिपरक भावना (व्यक्तित्व)
- दूसरा - वस्तुनिष्ठ भावना (परिवार, नागरिक समाज, राज्य)
- तीसरा - पूर्ण आत्मा (विकास के तीन चरण, जो कला, धर्म, दर्शन हैं)।
सिस्टम ख़त्म हो गया है.
इस प्रकार, दर्शनशास्त्र को न केवल मानव जाति के इतिहास में, बल्कि विश्व के संपूर्ण इतिहास में अंतिम और निर्णायक शब्द कहने का सम्मान प्राप्त है।
हेगेल के दर्शन का सामान्य निष्कर्ष दुनिया की तर्कसंगतता की मान्यता है: "जो कुछ भी वास्तविक है वह उचित है, जो कुछ भी उचित है वह वास्तविक है।"
- 3. एक विज्ञान के रूप में, एक प्रणाली के रूप में, तर्क के रूप में द्वंद्वात्मकता का निर्माण किया।
- ई) फ़्यूरबैक लुडविग एंड्रियास (1804-1872) - मानवशास्त्रीय भौतिकवाद के निर्माता।
- 1. धर्म और आदर्शवाद की आलोचना की और आदर्शवाद को तर्कसंगत धर्म कहा।
- 2. एल. फ़्यूरबैक की प्रणाली में विषय संज्ञानात्मक सोच नहीं है और न ही "पूर्ण आत्मा", शारीरिक, आध्यात्मिक और सामान्य विशेषताओं की एकता में एक क्षेत्रीय व्यक्ति है।
- 3. मनुष्य प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। प्रकृति आत्मा का आधार है। यह एक नए दर्शन का आधार भी होना चाहिए, जो मनुष्य के सांसारिक सार को प्रकट करने के लिए बनाया गया है।
- स्पिरकिन ए.जी.दर्शन // . - मॉस्को: सोवियत इनसाइक्लोपीडिया, 1977. - टी. 27. - एस. 412-417।
- ई.गुब्स्की, जी.कोरेबलेवा, वी.लुचेंकोदार्शनिक विश्वकोश शब्दकोश. - मॉस्को: इन्फ्रा-एम, 2005. - 576 पी। - 10,000 प्रतियां. - आईएसबीएन 5-86225-403-एक्स
- अलेक्जेंडर ग्रिट्सानोवनवीनतम दार्शनिक शब्दकोश. - मिन्स्क: स्काकुन, 1999. - 896 पी। - 10,000 प्रतियां. - आईएसबीएन 985-6235-17-0
- रॉबर्ट ऑडीदर्शन // डोनाल्ड एम. बोरचर्टदर्शनशास्त्र का विश्वकोश. - थॉमसन और गेल, 2006. - टी. 7. - एस. 325-337। - आईएसबीएन 0-02-865787-एक्स।
- दर्शनशास्त्र का ऑक्सफ़ोर्ड साथी / टेड होन्डेरिच। - नया संस्करण। - ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005। - 1060 पी। - आईएसबीएन 0-19-926479-1
परिचयात्मक साहित्य
रूसी में- पी.वी. अलेक्सेव, ए.वी. पैनिनदर्शन। - तीसरा संस्करण। - मॉस्को: प्रॉस्पेक्ट, 2005। - 604 पी। - 5000 प्रतियां. - आईएसबीएन 5-482-00002-8
- बी रसेलपश्चिमी दर्शन का इतिहास = पश्चिमी दर्शन का इतिहास. - मॉस्को: एमआईएफ, 1993. - टी. आई. - 512 पी। - 10,000 प्रतियां. - आईएसबीएन 5-87214-012-6
- बी रसेलपश्चिमी दर्शन का इतिहास = पश्चिमी दर्शन का इतिहास. - मॉस्को: एमआईएफ, 1993. - टी. II. - 446 पी. - 10,000 प्रतियां. - आईएसबीएन 5-87214-012-6
- एम.एन. रोसेंकोदर्शनशास्त्र का विषय. आधुनिक दर्शन के एक वैचारिक और पद्धतिगत सिद्धांत के रूप में मानवकेंद्रितवाद। // यु.एन. सोलोनिन और अन्य।आधुनिक दर्शन के मूल सिद्धांत. - सेंट पीटर्सबर्ग: लैन, 1999. - एस. 3-19। - आईएसबीएन 5-8114-0100-0.
- जैसा। कोलेनिकोव ऐतिहासिक प्रकारदर्शन // यु.एन. सोलोनिन और अन्य।आधुनिक दर्शन के मूल सिद्धांत. - सेंट पीटर्सबर्ग: लैन, 1999. - एस. 20-110। - आईएसबीएन 5-8114-0100-0.
- ए.ए. साइशेवदर्शन के मूल सिद्धांत. - मॉस्को: अल्फ़ा एम, 2010. - 368 पी। - 1500 प्रतियां. - आईएसबीएन 978-5-98281-181-3
- ब्रुक नोएल मूर, केनेथ ब्रुडरदर्शन। विचारों की शक्ति. - छठा संस्करण। - मैक ग्रा हिल, 2005. - 600 पी। - आईएसबीएन 0-07-287603-4
- एडवर्ड क्रेगदर्शन // निगेल वारबर्टनदर्शन। बेसिक रीडिंग.. - रूटलेज, 2005. - एस. 5-10। - आईएसबीएन 0-203-50642-1।
- रोडोल्फ गाशेसोच का सम्मान: आलोचना, सिद्धांत, दर्शन। - पहला संस्करण। - स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006. - 424 पी। - आईएसबीएन 0804754233
- रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दार्शनिक सोच की उत्पत्ति // रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दर्शन का कोलंबिया इतिहास। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. - एस. 1-5। - आईएसबीएन 0-231-10128-7।
दार्शनिक विद्यालयों पर विषयगत साहित्य
प्रारंभिक यूनानी दर्शन
- ए.आई. ज़ैतसेवसोफ़िस्ट // वी.एस. अंदर आएंआईएसबीएन 978-5-244-01115-9।
- कैथरीन ओसबोर्नप्रीस्कोक्रेटिक दर्शन। एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय. - ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004. - 146 पी। - आईएसबीएन 0-19-284094-0
- थॉमस एम. रॉबिन्सनपूर्व-सुकराती दार्शनिक // रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दर्शन का कोलंबिया इतिहास। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. - एस. 6-20। - आईएसबीएन 0-231-10128-7।
- थॉमस एम. रॉबिन्सनसोफ़िस्ट // रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दर्शन का कोलंबिया इतिहास। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. - एस. 20-23। - आईएसबीएन 0-231-10128-7।
यूनानी शास्त्रीय दर्शन
- वी.एफ. एस्मसप्लेटो. - मॉस्को: थॉट, 1975. - 220 पी। - (अतीत के विचारक)। - 50,000 प्रतियां.
- ए एफ। लोसेव, ए.ए. ताहो गोदीप्लेटो. अरस्तू... - तीसरा संस्करण। - मॉस्को: यंग गार्ड, 2005। - 392 पी। - (ज़िंदगी अद्भुत लोग). - 5000 प्रतियां. - आईएसबीएन 5-235-02830-9
- ए एफ। लोसेवप्लेटो का जीवन और रचनात्मक पथ // प्लेटो. चार खंडों में संकलित रचनाएँ. - मॉस्को: थॉट, 1994. - टी. 1. - एस. 3-63. - आईएसबीएन 5-244-00451-4।
प्राचीन भारतीय दर्शन
- वीसी. शोखिनभारतीय दर्शन // वी.एस. अंदर आएंआईएसबीएन 978-5-244-01115-9।
- डी.बी. ज़िल्बरमैन, ए.एम. पियाटिगोर्स्कीदर्शनशास्त्र [भारत में] // महान सोवियत विश्वकोश. - मॉस्को: सोवियत इनसाइक्लोपीडिया, 1972. - टी. 10. - एस. 221-223।
- मुकदमा हैमिल्टनभारतीय दर्शन: एक अत्यंत संक्षिप्त परिचय। - ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001. - 168 पी। - आईएसबीएन 0192853740
- कार्ल पॉटरभारतीय दर्शन // डोनाल्ड एम. बोरचर्टदर्शनशास्त्र का विश्वकोश. - थॉमसन और गेल, 2006. - वी. 4. - एस. 623-634। - आईएसबीएन 0-02-865784-5।
- वीसी. शोखिनभारतीय दर्शन. श्रमण काल. - सेंट पीटर्सबर्ग: सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी पब्लिशिंग हाउस, 2007। - 424 पी। - 1000 प्रतियां. - आईएसबीएन 978-5-288-04085-6
- वीसी. शोखिनभारतीय दर्शनशास्त्र के विद्यालय. गठन काल. - मॉस्को: पूर्वी साहित्य, 2004. - 416 पी। - (पूर्वी दर्शन का इतिहास)। - 1200 प्रतियाँ। - आईएसबीएन 5-02-018390-3
प्राचीन चीनी दर्शन
- वी.जी. बुरोवा, एम.एल. टिटारेंकोदर्शन प्राचीन चीन // प्राचीन चीनी दर्शन: 2 खंडों में.. - मॉस्को: थॉट, 1972. - टी. 1. - एस. 5-77.
- ए.आई. कोबज़ेवचीनी दर्शन // वी.एस. अंदर आएंन्यू फिलॉसॉफिकल इनसाइक्लोपीडिया: 4 खंडों में - मॉस्को: थॉट, 2010. - खंड 2. - आईएसबीएन 978-5-244-01115-9।
- लिविया कोह्नदाओवाद हैंडबुक। - बोस्टन: ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स, 2000. - 954 पी। - (हैंडबुक ऑफ ओरिएंटल स्टडीज / हैंडबच डेर ओरिएंटलिस्क)। - आईएसबीएन 90-04-11208-1
- विंग-त्सिट चानचीनी दर्शन: अवलोकन // डोनाल्ड एम. बोरचर्टदर्शनशास्त्र का विश्वकोश. - थॉमसन और गेल, 2006. - वी. 2. - एस. 149-160। - आईएसबीएन 0-02-865782-9।
- क्वांग-लोई शुनचीनी दर्शन: कन्फ्यूशीवाद // डोनाल्ड एम. बोरचर्टदर्शनशास्त्र का विश्वकोश. - थॉमसन और गेल, 2006. - वी. 2. - एस. 170-180। - आईएसबीएन 0-02-865782-9।
- चाड हेन्सनचीनी दर्शन: दाओवाद // डोनाल्ड एम. बोरचर्टदर्शनशास्त्र का विश्वकोश. - थॉमसन और गेल, 2006. - वी. 2. - एस. 184-194। - आईएसबीएन 0-02-865782-9।
- बो मौचीनी दर्शन: भाषा और तर्क // डोनाल्ड एम. बोरचर्टदर्शनशास्त्र का विश्वकोश. - थॉमसन और गेल, 2006. - वी. 2. - एस. 202-215। - आईएसबीएन 0-02-865782-9।
यूरोप का मध्यकालीन दर्शन
- चानिशेव ए.एन.प्राचीन और मध्यकालीन दर्शन पर व्याख्यान का पाठ्यक्रम। - मॉस्को: हायर स्कूल, 1991. - 512 पी। - 100,000 प्रतियां। - आईएसबीएन 5-06-000992-0
- सोकोलोव वी.वी.मध्यकालीन दर्शन. - मॉस्को: हायर स्कूल, 1979. - 448 पी। - 40,000 प्रतियां.
- एस.एस. नेरेटिनामध्यकालीन यूरोपीय दर्शन // वी.एस. अंदर आएंन्यू फिलॉसॉफिकल इनसाइक्लोपीडिया: 4 खंडों में - मॉस्को: थॉट, 2010. - खंड 4. - आईएसबीएन 978-5-244-01115-9।
- डेसमंड पॉल हेनरीमध्यकालीन और प्रारंभिक ईसाई दर्शन // डोनाल्ड एम. बोरचर्टदर्शनशास्त्र का विश्वकोश. - थॉमसन और गेल, 2006. - वी. 6. - एस. 99-107। - आईएसबीएन 0-02-865786-1।
- जी.ए. स्मिरनोवओकेकैम // वी.एस. अंदर आएंनया दार्शनिक विश्वकोश: 4 खंडों में - मॉस्को: थॉट, 2010. - आईएसबीएन 978-5-244-01115-9।
निकट पूर्व का मध्यकालीन दर्शन
- ई.ए. फ्रोलोवाअरब-मुस्लिम दर्शन का इतिहास: मध्य युग और आधुनिक समय। - मॉस्को: इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी आरएएस, 2006। - 199 पी। - 500 प्रतियां. - आईएसबीएन 5-9540-0057-3
- केसिया अली, ओलिवर लीमैनइस्लाम: प्रमुख अवधारणाएँ। - न्यूयॉर्क: रूटलेज, 2007. - 2000 पी। - आईएसबीएन 0415396387
- ई.ए. फ्रोलोवामध्य युग में अरब-इस्लामी दर्शन // एम.टी. स्टेपैनिएंट्सपूर्वी दर्शन का इतिहास. - मॉस्को: इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी आरएएस, 1998. - एस. 72-101। - आईएसबीएन 5-201-01993-5।
- कोलेट सीरतमध्यकालीन यहूदी दर्शन का इतिहास = मध्य युग में यहूदी दर्शन का इतिहास। - मॉस्को: ब्रिजेज़ ऑफ़ कल्चर, 2003. - 712 पी। - (बिब्लियोथेका जुडाइका। आधुनिक शोध)। - 2000 प्रतियां. - आईएसबीएन 5-93273-101-एक्स
भारत और सुदूर पूर्व का मध्यकालीन दर्शन
- जी.ए. तकाचेंकोचीन का मध्यकालीन दर्शन // एम.टी. स्टेपैनिएंट्सपूर्वी दर्शन का इतिहास. - मॉस्को: इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी आरएएस, 1998. - एस. 49-71। - आईएसबीएन 5-201-01993-5।
- वीसी. शोखिनभारत का मध्यकालीन दर्शन // एम.टी. स्टेपैनिएंट्सपूर्वी दर्शन का इतिहास. - मॉस्को: इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी आरएएस, 1998. - एस. 21-48। - आईएसबीएन 5-201-01993-5।
पुनर्जागरण का दर्शन
- वी. शेस्ताकोवपुनर्जागरण का दर्शन और संस्कृति। यूरोप की सुबह. - सेंट पीटर्सबर्ग: नेस्टर-इतिहास, 2007. - 270 पी। - 2000 प्रतियां. - आईएसबीएन 978-5-59818-7240-2
- ओह। गोर्फंकेलपुनर्जागरण का दर्शन. - मॉस्को: हायर स्कूल, 1980. - 368 पी। - 50,000 प्रतियां.
नये युग का दर्शन
- कार्ल अमेरिकासइम्मैनुएल कांत // रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दर्शन का कोलंबिया इतिहास। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. - एस. 494-502। - आईएसबीएन 0-231-10128-7।
- रिचर्ड एच. पॉपकिनफ्रांसीसी ज्ञानोदय // रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दर्शन का कोलंबिया इतिहास। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. - एस. 462-471। - आईएसबीएन 0-231-10128-7।
- हैरी एम. ब्रैकेनजॉर्ज बर्कले // रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दर्शन का कोलंबिया इतिहास। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. - एस. 445-452। - आईएसबीएन 0-231-10128-7।
- यूएन टिंग लाईतर्क के युग में चीन और पश्चिमी दर्शन // रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दर्शन का कोलंबिया इतिहास। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. - एस. 412-421। - आईएसबीएन 0-231-10128-7।
महाद्वीपीय दर्शन
- साइमन क्रिचलीमहाद्वीपीय दर्शन: एक बहुत संक्षिप्त परिचय। - ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001. - 168 पी। - आईएसबीएन 0-19-285359-7
- चार्ल्स ई. स्कॉटइक्कीसवीं सदी के मोड़ पर महाद्वीपीय दर्शन // रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दर्शन का कोलंबिया इतिहास। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. - एस. 745-753। - आईएसबीएन 0-231-10128-7।
- थॉमस नेननमहाद्वीपीय दर्शन // डोनाल्ड एम. बोरचर्टदर्शनशास्त्र का विश्वकोश. - थॉमसन और गेल, 2006. - वी. 2. - एस. 488-489। - आईएसबीएन 0-02-865782-9।
- बीसवीं सदी के फ्रेंच विचार का कोलंबिया इतिहास / लॉरेंस डी. क्रिट्ज़मैन, ब्रायन जे. रेली। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006। - 788 पी। - आईएसबीएन 978-0-231-10791-4
- पीटर सिंगरमार्क्स: एक बहुत संक्षिप्त परिचय. - ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001. - 120 पी। - आईएसबीएन 0-19-285405-4
- फ्रांज पीटर हग्डाहलउत्तरसंरचनावाद: डेरिडा और फौकॉल्ट // रिचर्ड एच. पॉपकिनपश्चिमी दर्शन का कोलंबिया इतिहास। - न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. - एस. 737-744। - आईएसबीएन 0-231-10128-7।
- एलेन सोकल, जीन ब्रिकमोंटबौद्धिक तरकीबें. उत्तर आधुनिक दर्शन की आलोचना = फैशनेबल बकवास। उत्तर आधुनिक बुद्धिजीवी "विज्ञान का दुरुपयोग। - मॉस्को: हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल बुक्स, 2002। - 248 पी. - 1000 प्रतियां - आईएसबीएन 5-7333-0200-3
- एन.वी.मोत्रोशिलोवा